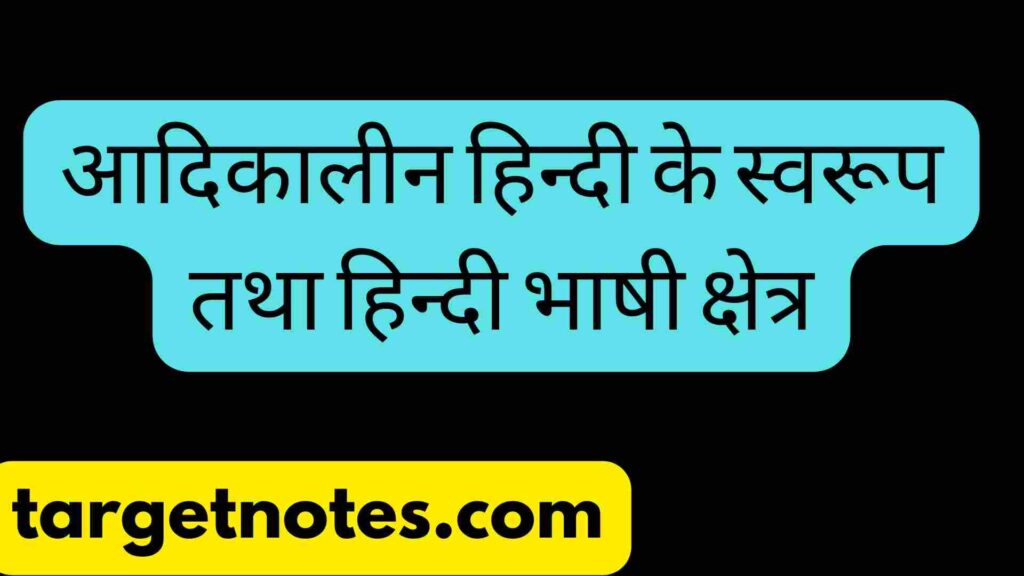
Contents
आदिकालीन हिन्दी के स्वरूप तथा हिन्दी भाषी क्षेत्र पर प्रकाश डालिए।
हिन्दी के उद्भव तथा ‘हिन्दी’ शब्द के अर्थ और उसके क्षेत्र विस्तार को लेकर काफी विवाद चलता रहा है। हिन्दी का एक अर्थ किया जाता है- खड़ी बोली। केवल खड़ी बोली को हिन्दी मानने वाले विद्वान हिन्दी साहित्य का इतिहास लगभग सौ वर्षों का ही मानते हैं। उनका मानना है कि हिन्दी के नाम पर जो एक हजार वर्षो से भी अधिक प्राचीन इतिहास तैयार किया गया है और खड़ी बोली के अतिरिक्त बज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि ही नहीं राजस्थानी साहित्य को भी घसीटा गया है तथा छात्रों को डिंगल-पिंगल का साहित्य पढ़ने को विवश किया जाता है यह मात्र हिन्दी के अन्य भक्तों का अन्याय है तथा उनकी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का परिचायक है। इनका तर्क है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्र का विद्यार्थी जब हिन्दी सीखने आता है। तो खड़ी बोली के ही इतिहास अथवा साहित्य का अध्ययन करना चाहता है क्योंकि जीवन में उसका सम्बन्ध खड़ी बोली से ही रहने की सम्भावना रहती है। उसे अन्य बोलियों के साहित्य को पढ़ने के लिए विवश करना उस पर अनावश्यक बोझ डालना है। प्रगतिशील आलोचक शिवदानसिंह चौहान का मत है-“पंजाबी, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, हरियानी, कुमायूँनी, डोंगरी, गढ़वाली आदि और चाहे कोई हों पर हिन्दी (खड़ी बोली) नहीं है।”
हिन्दी के सम्बन्ध में दूसरा भ्रम भाषा वैज्ञानिकों, विशेष रूप से मियर्सन के द्वारा फैलाया गया है। वह हिन्दी सर्वेक्षण में हिन्दी के दो रूप मानते हैं-पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी। पश्चिमी हिन्दी को पाँच बोलियों-खड़ी बोली, बाँगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुन्देली तथा पूर्वी हिन्दी को तीन बोलियों-अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में विभक्त किया। इस प्रकार भाषा की दृष्टि से वह गोरखपुर और वाराणसी मंडल को छोड़कर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ भाग को हिन्दी का क्षेत्र मानते हैं। लेकिन अपने दूसरे ग्रन्थ- ‘उत्तरी हिन्दुस्तान का आधुनिक देशी भाषा साहित्य का इतिहास’ में वह केवल खड़ीबोली को हिन्दी मानते हैं। उनके मत से यह “यह भाषा यूरोपीय लोगों द्वारा हिन्दी कही गयी और सम्पूर्ण भारतवर्ष में हिन्दुओं की राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गयी, क्योंकि उसका अभाव था और इसने उसे पूरा कर दिया। यह सम्पूर्ण उत्तरी भारत में गद्य की सर्वस्वीकृत भाषा हो गयी। किन्तु यह कहीं की देश भाषा नहीं थी। अतः इसका काव्य के क्षेत्र में कहीं भी सफल प्रयोग नहीं हो सका।” यह सम्भव हो सकता है कि हिन्दी नाम भले ही परवर्ती हो किन्तु हिन्दी भाषा नवीन नहीं है। उनकी यह मान्यता कि अंग्रेजों के आगमन के बाद उनके सुझाव पर राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी नामक एक कृत्रिम भाषा को गढ़ लिया गया वैसे ही अनर्गल है जैसे कोई कहे कि मुसलमानों के आगमन के बाद ही हिन्दू जाति अस्तित्व में आयी। वस्तुतः खड़ी बोली का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि ब्रज, अवधी आदि अन्य बोलियों का। भाषा वैज्ञानिकों ने उसका भी उद्भव शौरसेनी, प्राकृत या अपभ्रंश से माना है। 10वीं- 11वीं शताब्दी के अपभ्रंश तथा देशी भाषा के साहित्य में खड़ी बोली के तत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। अकबर के समकालीन गंग कवि ने ‘चन्द छन्द बरनन की महिमा’ नामक गद्य की पुस्तक खड़ी बोली में लिखा था। प्रियर्सन और शिवदानसिंह चौहान के समान ही सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय का भी अभिमत है- “वह हिन्दी बोलने वालों की संख्या 40-50 लाख ही मानते हैं तथा शेष हिन्दी क्षेत्र को मैथिली, गायत्री, भोजपुरी, कौशली, राजस्थानी, भीरी, पहाड़ी आदि भाषाओं में विभक्त कर देते हैं।”
सच तो यह है कि सुनीति बाबू ने हिन्दी क्षेत्र में जिन स्वतन्त्र भाषाओं की कल्पना की है वे हिन्दी की ही बोलियाँ हैं। भाषा और बोली में भेद न करने के कारण ही यह भ्रम फैला है। भाषा में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं- (i) केन्द्रापगामी (i) केन्द्राभिगामी । व्यक्ति की प्रवृत्ति केन्द्रापगामी होती है और समाज की प्रवृत्ति केन्द्राभिगामी होती है। प्रथम प्रवृत्ति से बोली का जन्म होता है और दूसरी से भाषा का विकास। वस्तुतः दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं है। एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियाँ व्यवहत होती हैं। व्यवहार में भाषा वह तत्व है जो एक प्रकार की भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्प्रेषण का माध्यम है। इस प्रकार भाषा का अर्थ एक जातीय बोलियों का समूह है। इन्हीं बोलियों में से कोई एक बोली राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से व्यापक रूप धारण करके शासन, साहित्य और शिक्षा का माध्यम बन जाने पर भाषा की पर्यायवाची बन जाती है और इन कारणों के अभाव में वह पुनः बोली रह जाती है और उसके स्थान पर कोई दूसरी बोली उस भाषा के पर्याय के रूप में स्वीकृत हो जाती है। बोली को भाषा में परिणत करने का सबसे बड़ा साधन होता है-सम्पर्क। मध्य काल में ब्रजमण्डल) की बोली भक्तों और अन्य कवियों के द्वारा अपनायी जाने के कारण न केवल पूरे हिन्दी क्षेत्र-राजस्थान से बिहार तक फैल गयी बल्कि बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र में भी उसमें रचनाएँ होने लगीं। आधुनिक काल में मेरठ डिवीजन की खड़ी बोली ने उसी प्रकार शासन, साहित्य और शिक्षा का माध्यम बनने पर न केवल ब्रजभाषा का स्थान ले लिया है बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में पूरे देश के लिए स्वीकृत हो चुकी है। भाषा की विभिन्न बोलियों और स्वतन्त्र भाषाओं में एक अन्तर यह भी होता है कि विभिन्न भाषा-भाषी एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते जबकि एक भाषा क्षेत्र में विभिन्न बोलियों का प्रयोग करने वाले लोग एक दूसरे की वाणी सहज ही समझ लेते हैं। राजस्थान से बिहार तक की भाषा एक है। इस पूरे क्षेत्र का निवासी घर में अथवा स्थानीय मित्रों में भले ही बज, अवधी, भोजपुरी, मराठी या राजस्थानी, बाँगरू या पहाड़ी आदि बोलता हो किन्तु शिष्ट समाज में वह खड़ी बोली हिन्दी का ही प्रयोग करता है जबकि गुजराती, बंगाली, मराठा और दक्षिण वासी खड़ी बोली का व्यवहार नहीं करते। इसी प्रकार शिक्षा, साहित्य और शासन में बोलियों का प्रयोग न होकर मुख्य भाषा का ही प्रयोग होता है।
हिन्दी की सीमा के सम्बन्ध में एक दूसरा पक्ष भी है जहाँ एक ओर कुछ लोग हिन्दी को केवल खड़ी बोली तक ही सीमित रखना चाहते हैं, वहाँ दूसरी ओर अन्य लोग हिन्दी के अन्तर्गत न केवल राजस्थान से बिहार तक की सभी बोलियों के साहित्य को अपनाने की बात करते हैं अपितु उर्दू, पंजाबी, गुजराती और दक्खिनी हिन्दी या रेख्ता के साहित्य को भी हिन्दी के अन्तर्गत समाविष्ट करना चाहते हैं। भारतीय हिन्दी परिषद् द्वारा प्रकाशित ‘हिन्दी साहित्य-द्वितीय खण्ड’ में न केवल उर्दू के मीर, सैदा, गालिब आदि का उल्लेख है बल्कि पंजाबी के गुरुनानक, गुरुगोविन्द सिंह और दक्खिनी हिन्दी के ख्वाजा बन्दे निवाज, कुली कुलुफशाह, वजही आदि को भी सम्मिलित कर लिया गया है।
हिन्दी-उर्दू का विवाद काफी पुराना है। वह सर सैयद अहमद खाँ के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हो गया था। अंग्रेजों के शासन काल में उर्दू समर्थकों के प्रभाव के कारण हिन्दी को बहुत क्षति भी पहुँची। इसी प्रकार स्वाधीनता आन्दोलन के समय भी भाषा का प्रश्न उठा था और काँग्रेस ने हिन्दी को स्वतन्त्र भारत की राष्ट्र भाषा भी स्वीकार कर लिया था किन्तु कुछ ही वर्षों बाद मुसलमानों के विरोध के कारण हिन्दी, उर्दू का विवाद उठ खड़ा हुआ तब गाँधी जी और उनके अनुयायियों ने हिन्दी-उर्दू मिश्रित रूप ‘हिन्दुस्तानी’ को अपनाये जाने पर जोर दिया किन्तु समन्वय का यह प्रयत्न विफल रहा। इतिहास के रोचक और कुछ करुण अन्तर्विरोधों में से एक यह है कि तराना-ए-हिन्दी के गायक, अपने को हिन्दी कहने वाले और अपने वतन को हिन्दुस्तान मानने वाले विख्यात शायर और मनीषी डॉ० इकबाल काल क्रम में पाकिस्तान की योजना के आरम्भिक प्रस्तावकों में एक थे। पर यह अन्तर्विरोध का मूल गुण आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के प्रयोग में ‘विरुद्धों का सामंजस्य’ हिन्दू धर्म और हिन्दुस्तान की संस्कृति का आधारभूत तत्व है। यों अन्तर्विरोधों का होना और फिर उनका समन्वय एक प्रकार से संस्कृति मात्र का लक्षण है, उसकी जीवन्तता का प्रमाण है, पर हिन्दू धर्म और उससे जुड़ी तथा उसके सहारे विकसित संस्कृति में यह प्राण धारक तत्व रहा है जिसके होने से ही कवि सरल से लगते तराने में यह गहरी अनुभूति उसे हुई थी- “कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।” यह बात ध्यान से देखने पर हिन्दू मानसिकता की वह शक्ति है जो अनेक अन्तर्विराधों को अपने में समोये हुए है।
इन अन्तर्विरोधों को समोने की शक्ति हिन्दू मानस को शायद इसलिए मिली कि वह किसी धर्म ग्रन्थ विशेष और व्यक्तित्व विशेष पर अनिवार्यतः आस्था लाने का आदेश नहीं देता। इसलिए आस्तिक-नास्तिक, ब्राह्मण- शैव, मूर्तिपूजक और प्रतिमा-भंजक सब उसके प्रवाह में शामिल हैं। तब अन्तर्विरोधों का उपजना स्वाभाविक है और हिन्दू दिमाग धीरे-धीरे उनको शमन करने का आदी होता गया है। यहाँ धर्म संस्थागत नहीं बना वरन् एक आन्तरिक जिजीविषा का रूप हो गया। हिन्दू मानस के अनेक अन्तर्विरोधों में सबसे दिलचस्प है। सूक्ष्म अद्वैत दर्शन और जड़ीभूत जाति-व्यवस्था का सह-अस्तित्व । तत्व चिन्तन की सूक्ष्मतम भाव-भूमि अद्वैत की परिकल्पना में है जहाँ सम्पूर्ण यथार्थ एक ब्रह्म की सत्ता की ही विविधरूपा अभिव्यक्ति है। यह अद्वैत भावना हिन्दू दर्शन की विशिष्ट उपलब्धि है और इस रूप में अन्यत्र नहीं मिलेगी। वहीं जाति प्रथा का स्थूल रूप- जन्म पर आधारित, जाति के मूल अर्थ में हो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जातियों का जाल और वर्गीकरण इतना पूर्ण और व्यवस्थित है कि छन्द शास्त्र का प्रस्तार याद आ जाता है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह टिप्पणी- “हिन्दू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ़ लेती है। “- व्यंग नहीं व्यावहारिक सच है। एकत्व का परम रूप अद्वैत में और वैविध्य की बाहर जाति प्रथा में ये दोनों छोर हिन्दू व्यवस्था में बड़े इत्मीनान के साथ समाये हुए हैं। कुछ ऐसा ही अन्तर्विरोध भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं में मिलता है। एक ओर रस-सिद्धान्त सूक्ष्म चिन्तन है जो अपनी ऊंचाइयों में दर्शन की कोटि तक पहुँचता है और दूसरी ओर अलंकारों और ध्वनियों का स्थूल तौर पर विभाजन और वर्गीकरण है जो बाबू गुलाब राय को हिन्दू-जाति-प्रथा का स्मरण दिलाता है। ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में उन्होंने “या अल्लाह। गौड़ों में भी और।” वाला किस्सा याद किया है।
भारतवर्ष के दो आदि काव्य ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ अपनी परिकल्पना में एक दूसरे के विरोधी हैं। एक आदर्श की चरम गाथा है तो दूसरा यथार्थ का नग्न रूप। कथा का मूल ढाँचा दोनों जगह भारतीय हिन्दू परिवार में भाइयों के आपसी सम्बन्ध पर टिका हुआ है, लेकिन इन सम्बन्धों की दिशा अलग-अलग हैं। हिन्दू मानस के चरम अन्तर्विरोध का रूप यहाँ देखने को मिलता है। हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि धर्म वस्तुतः वह है जो अन्तर्विराधों को धारण करने की सामर्थ्य रखता है। धारण करने की इस शक्ति ने भारतीय संस्कृति को प्रबल महणशीलता और प्रवाहमानता दी है। यह सत्य है कि इस संस्कृति का मूलाधार आर्य संस्कृति रही लेकिन बहुत बड़ा अंश आर्येतर सभ्यता का है, आगमों का है, बौद्ध, जैन और सिक्खों का है तत्पश्चात् इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रभाव है। यह सब मिलाकर भारतीय संस्कृति की धारा बनती है। अन्तर्विरोधों की द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया में यह धारा इतने लम्बे समय तक गतिशील बनी रही है। विविध कालों में हिन्दुओं में ऐसे देवता ही अधिक लोकप्रिय हुए हैं जिनमें अन्तर्विराधों को धारण करने की क्षमता थी। इन्द्र में एक ओर योद्धा तो दूसरी ओर संगीत और कला प्रेमी: शिव-सबसे बड़े योगी तो वैसे ही भोगी, ज्ञानी तो भोलानाथ भी; कृष्ण में प्रेमी कूटनीतिज्ञ और दार्शनिक के परस्पर विरोधी पक्ष ऐसे घुल-मिल गये हैं कि सहसा उनके विरोधत्व का आभास ही नहीं होता। इन विरोधों और उनकी समरसता के बीच से इस देश के मनीषियों और दार्शनिकों ने जीवन की एक समय, समृद्ध और सम्पूर्ण प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाही है और यही हिन्दू धर्म का मूल चरित्र है।
हिन्दी भाषा की प्रकृति इसी चरित्र से जुड़ी हुई है। भौगोलिक विस्तार के अनेक जनपदों और व्यवहत अठारह बोलियों के वैविध्य को जिनमें से कई व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे की विरोधी विशेषताओं से युक्त कही जा सकती है, हिन्दी भाषा से बड़े सहज भाव से धारण करती है। हिन्दी के स्वरूप के सम्बन्ध में इसीलिए वैचारिक द्वैत की भावना ग्रियर्सन में जगह-जगह ‘दिखती है। ‘भाषा सर्वेक्षण’ के भूमिका भाग में वे लिखते हैं-“इस प्रकार यह कहा जाता है और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा के समस्त कांठे में, बंगाल और पंजाब के बीच अपनी अनेक स्थानीय बोलियों सहित केवल एक मात्र प्रचलित भाषा हिन्दी ही है। एक दृष्टि से यह ठीक ही है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्वत्र हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी शासन की भाषा है और ग्रामीण स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस क्षेत्र के लोग द्विभाषा-भाषी हैं, अतएव व्यवहार में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती और ये लोग नहीं चाहते कि शासन कार्य के लिए अनेक भाषाएँ स्वीकार कर कठिनाई उत्पन्न की जाय। यह सब होते हुए भी तथाकथित हिन्दी की इन बोलियों की जब भाषाशास्त्री परीक्षा करता है तो इनके मुहावरों तथा गठन में उसे अत्यधिक अंतर मिलता है।” डॉ० मियर्सन के काफी पहले विलियम कैरे ने सन् 1815 में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये थे। एक और हिन्दी क्षेत्र की बोलियों में शब्दावली की समानता होने पर भी उन्हें रूप-तन्त्र की भिन्नता प्रतीत हुई और दूसरी ओर हिन्दी के विस्तार के प्रति बड़े आश्वस्त भाव से उन्होंने पहली नजर में लिखा है-“इस बोली से मैं सारे हिन्दुस्तान को समझा सकूँगा।” यहाँ यह स्मरण रखना है कि करे का भाषा सर्वेक्षण अपने ढंग का पहला प्रयास है और बाइबिल के अनुवादों के सिलसिले में उन्होंने हिन्दी क्षेत्र की बोलियों का गहराई के साथ परीक्षण किया था।
हिन्दी क्षेत्र की 18 बोलियाँ- पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुन्देली; पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत- अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बिहारी के अन्तर्गत-मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी के अन्तर्गत- मेवाती, अहीरवाटी, मालवी जयपुरी-हड़ौती, मारवाड़ी मेवाड़ी, पहाड़ी के अन्तर्गत पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी = 18 बोलियाँ] व्युत्पत्ति की दृष्टि से अलग-अलग अपभ्रंशों से विकसित हुई हैं। बोधगम्यता के सन्दर्भ में तो प्रियर्सन ने कहा है कि झांसी जिले के किसान अर्थात् बुन्देली बोलने वाले को गोरखपुर जिले के भोजपुरी बोलने वाले किसान से बात करने में कठिनाई होगी। व्याकरण के स्तर पर पश्चिमी हिन्दी, हिन्दी, पूरबी हिन्दी और भोजपुरी के अन्तर प्रसिद्ध है। पश्चिम की बोलियों में कर्ताकारक के लिए प्रयुक्त ‘ने’ परसर्ग पूर्व में अवधी और भोजपुरी में एकदम अनुपस्थित है। पश्चिम में भविष्यत् काल के लिए ‘ह’ तथा ‘य’ प्रत्यय है तो पूरब में ‘ब’ दूसरी ओर पूरब के भूतकाल में प्रयुक्त “अल’, ‘इल’ प्रत्यय पश्चिम की बोलियों में नहीं हैं। ‘अ’ स्वर का उच्चारण भोजपुरी में जिस रूप में है वह बंगला आदि पूरबी भाषाओं के निकट है बजाय पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र की बोलियों के। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर प्रियर्सन ने लिखा है- “तथाकथित हिन्दी की बोलियाँ।” इस उक्ति से एक बात स्पष्ट होती है। कि प्रियर्सन अपने भाषा वैज्ञानिक विचार-क्रम में इन बोलियों को एक भाषा से सम्बद्ध नहीं मानते। उनके सर्वेक्षण में हिन्दी क्षेत्र की पाँच उपभाषाएँ- पश्चिमी हिन्दी, पूरबी हिन्दी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी किसी एक स्थान पर विवेचित न होकर सर्वेक्षण की पाँच अलग-अलग जिल्दों में क्रमश: 9:1, 6:5: 29: 2, 4- वर्णित हुई हैं तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में उन्होंने भीतरी, बाहरी तथा बीच की तीनों भाषाओं में हिन्दी क्षेत्र की बोलियों को रखा है अर्थात् प्रियर्सन के अनुसार हिन्दी क्षेत्र की बोलियों की विशेषताएँ सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं के समान हैं। तब यह अकारण नहीं है कि इन तीनों वृत्तों का केन्द्र उन्होंने पश्चिमी हिन्दी को माना है- “जब उन्हें भारतीय आर्य भाषा को किसी क्रम में रखना पड़ेगा तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की भाषा पश्चिमी हिन्दी को केन्द्र में रखना पड़ेगा।”
इसके बावजूद इन सारी बोलियों के समूह और संश्लेष को पहले भी ‘हिन्दी’ ‘हिन्दवी’, ‘हिन्दुई’ कहा जाता था और आज भी ‘हिन्दी’ कहा जाता है। कबीर और मुल्ला वजही, जायसो और तुलसी, सूर और मीराबाई, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मैथिलीशरण गुप्त, निराला और अज्ञेय समान रूप और समभाव से हिन्दी के कवि हैं। इनकी रचनाओं में हिन्दी की ही संवेदना व्यक्त हुई है। इसके पीछे अन्य कारण है जो भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम से कुछ अलग पड़ते हैं। एक तो हिन्दी क्षेत्र या प्राचीन मध्यदेश के जनपदों के बीच सामाजिक सम्बन्धों की स्थिति और सांस्कृतिक एकरूपता बराबर रही है। प्रियर्सन ने इस स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से पहचाना है। बिहारी के प्रसंग में वे लिखते हैं-“यहाँ तक कि रामायण महाकाव्य की रचना के युग में भी अयोध्या (आधुनिक अवध) के राजकुमार रामचन्द्र ने मिथिला अथवा आधुनिक बिहार की प्रसिद्ध राजकुमारी सीता के साथ विवाह किया था। बिहार का मुख सदैव उत्तर पश्चिम की ओर रहा, बंगाल की ओर से तो उस पर शत्रुतापूर्ण आक्रमण ही होते रहे। इन्हीं कारणों से लोग बिहारी भाषा को यू०पी० में प्रचलित हिन्दी का ही एक रूप मानते हैं किन्तु वास्तव में यह तथ्य के सर्वथा विपरीत है। बिहार तथा बंगाल में पारस्परिक चाहे जो दुर्भावना हो, बिहारी भाषा बंगला की बहन है और पश्चिम की बोली से उसका बहुत दूर का सम्बन्ध है।” जब भाषा वैज्ञानिक तथा सामाजिक साक्ष्यों के बीच वैषम्य उपस्थित होता है तो ग्रियर्सन अपनी मान्यता भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों को ही देते हैं। पर बिहार की भाषिक स्थिति इसी से प्रकट नहीं होती कि वहाँ की बोलियों का व्याकरण बंगला जैसा है, बल्कि इससे भी जुड़ी है कि वहाँ के निवासी अपनी काव्य-भाषा के लिए बजभाषा अथवा खड़ी बोली को आधार रूप में चुनते हैं और उनकी जातीय पाठ्य रचना तुलसीकृत रामचरित मानस है न कि कोई बँगला काव्य । यही काव्य-भाषा के महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। काव्य-भाषा का सम्बन्ध रचनाकार से ही नहीं होता और पाठक वर्ग से भी होता है। इस रूप में वह पूरे जनसमाज को परस्पर जोड़े रहता है। एक और जन बोली से वह शक्ति लेती है और दूसरी ओर उसे परिष्कार देती है। इस प्रकार किसी क्षेत्र की काव्य-भाषा वहाँ के समाज को प्रतिफलित करती है।
समूचे मध्यदेश की काव्य-भाषा का आधार हर युग में एक रहा है। कभी आरम्भ में वह खड़ी बोली था, तो कभी खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिला-जुला रूप फिर मध्यकाल में बजभाषा और अंशतः अवधी और अब आधुनिक काल में यह आधार फिर से खड़ी बोली हुआ है। कुमायूँ से सुमित्रानन्दन पन्त, बैसवाड़े से निराला, बजक्षेत्र से महादेवी वर्मा और भोजपुरी क्षेत्र से प्रसाद आकर एक खड़ी बोली के आधार पर उस नये काव्य आन्दोलन को जन्म देते हैं जो आधुनिक कविता की विशिष्टतम उपलब्धि बनता है। छायावादी कविता इराने बोली- क्षेत्रों के संस्कार अपने में समाहित किये हैं जो घुल-मिलकर एक काव्य भाषा में रचे गये हैं। हिन्दी क्षेत्र की भाषिक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह समान का काव्य भाषा का प्रयोग है। आधुनिक काल में इसे मध्यवेश अथवा हिन्दी प्रदेश की पहचान बनाने में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन तथा वासुदेव शरण अग्रवाल प्रमुख हैं। राजनीति क्षेत्र के विचारकों में डॉ० राममनोहर लोहिया का ध्यान इस ओर गया। उर्दूजों बोलचाल में खड़ी बोली का ही एक रूप है, हिन्दी काव्य-भाषा से अलग हो जाती है। लेकिन यह अलगाव साम्प्रदायिक धरातल पर कभी नहीं रहा। अलगाव का मात्र आधार यह रहा कि उर्दू दरबार से जुड़ी रही- यद्यपि बाजार से भी उसका सम्बन्ध बराबर बना रहा और हिन्दी विविध बोलियों के रूप में जनसाधारण में प्रयुक्त होती रही। इस प्रकार एक ही खड़ी बोली के दो रूप अलग ढंग से संस्कारित और प्रचारित हुए । कविता में यह संस्कार एकदम फर्क हो गया लेकिन यह अलगाव या फर्क हिन्दू-मुसलमान के आधार पर कभी नहीं हुआ। जायसी, रहीम, रसखान, आलम, कुतुबन जैसे मुसलमान हिन्दी में लिखते रहे तो हिन्दुओं में चक, सरशार, आनन्द नारायण, मुल्ला, फिराक उर्दू के श्रेष्ठ रचनाओं में स्थान पाते रहे। हिन्दी-उर्दू में अन्तर बोलचाल के सतर पर नहीं है, केवल साहित्य के स्तर पर है। कुछ तो भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से, कुछ छन्द-विधान को लेकर पर अधिकता काव्य भाषा की प्रयोग विधि में अन्तर के कारण। सांस्कृतिक और दरबारी अनुषंगों के ही होने से खड़ी बोली के दोनों रूपों-उर्दू और खड़ी बोली को हिन्दी लेखकों विशेषतः ब्रज भाषा के समर्थकों द्वारा ‘यामिनी’ कहकर सम्बोधित किया गया। यह अवमानना और तिरस्कारसूचक विशेषण उर्दू के लिए नहीं, खड़ी बोली के लिए था क्योंकि इसका सम्पर्क इस्लामी दरबार से था। इसके अलावा उर्दू ने वर्णिक या मात्रिक, भारतीय परम्परा के किसी छन्द विधान को स्वीकार नहीं किया फलस्वरूप काव्य भाषा को प्रयोग विधि के कारण भी उर्दू शैली में अलगाव आया। उर्दू की विशेषता यह थी कि वह उच्च संस्कृति से जुड़ी थी लेकिन अपने नाम के अनुरूप लश्कर के बाजार से भी। उर्दू काव्य भाषा में अर्थ क्षमता बोल-चाल के मुहावरे से उपजती है न कि कवियों द्वारा विकसित विशिष्ट विम्ब-विधान से उर्दू को हिन्दी की एक शैली मानने वाले विद्वज्जनों से एक अनुरोध है कि यदि उर्दू को हिन्दी में अन्तर्भुक्त करना है तो हिन्दी साहित्य के इतिहास में आमूल परिवर्तन कर समस्त उर्दू वाड्मय को हिन्दी के समकक्ष स्थान देना होगा जैसे कि ब्रज, अवधी आदि के साहित्य को दिया है। उर्दू के समान ही दक्खिनी हिन्दी को भी अपनाये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार भले ही आज राजनीतिक और अन्य कारणों से पंजाबी एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में स्थापित हो गयी है लेकिन सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में गुरुनानक और गुरू गोविन्द सिंह की वाणी और रचनाओं को सम्मिलित करना होगा क्योंकि इन गुरुओं ने अपनी रचनाओं की भाषा को हिन्दी से अलग नहीं मानते थे। लेकिन अब इसे विवेक, सौहार्द्रपूर्ण और प्रेमपूर्ण ढंग पर करना होगा, पंजाबी भाषियों के साथ ‘बिग ब्रदर’ के रूप में व्यवहार करके नहीं। तभी राष्ट्रीय एकता का सपना साकार होगा।
सच तो यह है कि साहित्यिक काल-विशेष का नामकरण उस मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर होना चाहिए जो उस काल के प्रमुख और अधिकांश कवियों को काव्यप्रेरणा देती रही है। भक्तिकाल नाम इसलिए उपयुक्त और संगत हैं कि उस काल के अधिकांश और प्रमुख कवियों की काव्य-रचना की मूल प्रेरक शक्ति भगवत्भक्ति रही। इसी प्रकार विक्रम की 16वीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रमुख और बहुसंख्यक कवियों की प्रेरणा उस काव्य-शैली से मिली थी जिसे संक्षेप में और अवितर्क रूप में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ‘रीति’ कहा था। इस प्रकार रीतिकाल नाम ही सर्वथा उपयुक्त है और हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अतिरिक्त डॉ० श्यामसुन्दर दास, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, डॉ० गुलाबदास तथा डॉ० भगीरथ मिश्र आदि विचारकों ने भी इसे रीतिकाल कहना अधिक युक्तिसंगत समझा है।
आदिकाल में मूल हिन्दी भाषी प्रदेश में हिन्दी रचनाओं का अभाव
हिन्दी भाषा के आदिकाल में मूल हिन्दी- भाषी प्रदेश के कवियों की रचनाएं प्राप्त नहीं होतीं, जो मिलती हैं वे या तो सीमांत प्रदेश में पाई जाती हैं या विकृत रूप में ही मिलती हैं। डॉ० हजारी प्रसाद ने उस समय के भारत के ऐतिहासिक सर्वेक्षण के आधार पर इस अभाव के कारण की गवेषणा की है, जो निम्नांकित है-
इस काल की पुस्तकें तीन प्रकार से सुरक्षित हुई हैं- (1) राज्याश्रय पाकर और राजकीय पुस्तकालयों में सुरक्षित रहकर, (2) सुसंगठित धर्म सम्प्रदाय का आश्रय पाकर और मठों-विहारों आदि के पुस्तकालय में शरण पाकर राज्याश्रय सबसे प्रबल साधन था। धर्म सम्प्रदाय का संरक्षण उसके बाद आता है। तीसरे प्रकार से जो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं वे बदलती रही हैं और लोक-पित्त की चंचल सवारी करती रही हैं। समय-समय पर उनमें परिवर्तन और परिवद्र्धन भी होता रहा है। आल्हा काव्य इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह बता सकना कठिन है कि आल्हा खंड का असली रूप क्या था ? इसके विपरीत उस समय के अन्य काव्य आल्हा काव्य के समान लोक-प्रीति का भाजन नहीं बन सके और अपना शुद्ध रूप लिए अस्त हो गये।
देशी भाषा की दूसरी पुस्तकें जैन सम्प्रदाय का आश्रय पाकर साम्प्रदायिक भंडारों में सुरक्षित रह गयी हैं। उनका शुद्ध रूप भी सुरक्षित रह गया। कुछ पुस्तकें बौद्ध धर्म का आश्रय पाकर बौद्ध नरपतियों की कृपा से बच गई थीं जो आगे चलकर हिन्दुस्तान के बाहर पाई जा सकी हैं, परन्तु जो पुस्तकें हिन्दू धर्म और हिन्दू नरेशों के संरक्षण में बची हैं वे अधिकांशतः संस्कृत में हैं।
मूल हिन्दी भाषा प्रदेश में हिन्दी रचनाओं का अभाव क्यों रहा, इसका कारण बताते हुए डॉ० साहब लिखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरान्त भी उसके सेनापति भंडि तथा उसके वंशज कुछ काल तक शासन करते रहे। नवीं शताब्दी के आरंभ में वर्धनों की शक्ति क्षीण हुई।
तीन शक्तियाँ- पूर्व के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट और पश्चिम के प्रतिहार कान्यकुब्ज की राज्यलक्ष्मी को हथियाने में प्रयत्नशील रहे किन्तु सफलता प्रतिहारों को ही मिली। इसके बाद लगभग दो शताब्दियों तक कान्यकुब्ज के प्रतिहार बड़े शक्तिशाली शासक बने रहे।
उस समय का मध्य देश राजनीतिक दृष्टि से बड़ा ही विक्षुब्ध था। उस समय के गहड़वार नरेश, चाहे वे दक्षिण से आये या पश्चिम से, वे बाहर के ही थे। उन्होंने काफी समय तक स्थानीय जनता से अपने आप को अलग रखा। वे वैदिक संस्कृति के उपासक थे और बाहर से बुला-बुलाकर अनेक ब्राह्मण-वंशों को काशी में बसा रहे थे। काशी में संस्कृत को इन लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया पर इनके यहाँ हिन्दी को प्रश्रय न मिल सका। जिस प्रकार गौड़ देश के पाल गुजरात के सोलंकी और मालवा के परमार देशी भाषा को प्रोत्साहन दे रहे थे। वैसा गहड़वारों के दरबार में नहीं हुआ। डॉ० हजारीप्रसाद इस उपेक्षा के कारणों का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं-“ये लोग बाहर से आये थे और देशीय जनता के साथ दीर्घ काल तक एक नहीं हो पाये थे। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मध्य देश में जिस संरक्षणशील धारा की प्रतिष्ठा थी उसमें संस्कृत भाषा और वर्जनशील ब्राह्मण व्यवस्था से अधिकाधिक चिपटा रहना ही स्थानीय जनता की दृष्टि से ऊंचा उठने का साधन रहा हो।” आरंभ में गहड़वार नरेश स्थानीय जनता से अलग बने रहे, परन्तु शनैः-शनैः यह प्रवृत्ति कम होने लगी। गहड़वार नरेश गोविन्दचन्द्र के सभा-पंडित दामोदर भट्ट ने राजकुमारों को काशी की भाषा सिखाने का प्रयत्न किया और इस प्रकार धीरे-धीरे देशी भाषा को इस दरबार में प्रोत्साहन मिलने लगा। दुर्भाग्यवश जयचन्द के अस्त होने के साथ इस प्रोत्साहन और प्रवृत्ति का अंत हो गया। अब समस्त उत्तरी भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं की विजयपताका फहराने लगी। इन नये शासकों को देशी जनता के साथ एक होने में और भी अधिक समय लगा।
गहड़वारों के शासन काल में समूचा हिन्दी प्रदेश स्मार्त धर्मानुयायी था। जब गहड़वारों का प्रभाव क्षीण हो गया और अजमेर कालिंजर आदि राज्य स्वतंत्र हो गये तो उन राज्यों में भी स्मार्त धर्म की प्रबलता रही। इस समय शैव मत का दबदबा था। नाथ योगियों, रसेश्वर मत के मानने वाले रस सिद्धों और मन्त्र-तन्त्र में विश्वास रखने वाले शक्ति-साधकों का इन क्षेत्रों में बड़ा जोर था। पर इन शैव साधकों के संगठित मत नहीं थे और न ही इनका देशी भाषा के प्रति कोई विशेष अनुराग था। इसके अतिरिक्त ये जनता के प्रति भी तटस्थ बने रहे। केवल यह ही नहीं, तब की जनता इनसे अतीव भयभीत थी। अतः स्पष्ट है कि इनके द्वारा प्रणीत रचनायें जनप्रिय नहीं हो सकती थीं। कुछ थोड़ी सी पुस्तकें इन योगियों की मिल जाती हैं पर एक तो उन्हें जैन पुस्तकों के समान संगठित भंडारों का आश्रय नहीं मिला, दूसरे वे आल्हा आदि की भाँति लोक-मनोहर भी नहीं हो सकीं। इनकी रक्षा का भार सम्प्रदाय के कुछ अशिक्षित साधुओं पर रहा। इन रचनाओं को प्रामाणिक रूप में सुरक्षित रखने का प्रयत्न नहीं किया गया। परवर्ती साहित्य में इन योगियों का दो रूपों में उल्लेख मिलता है- (1) सूफी कवियों की कथा में नाना प्रकार की सिद्धियों के आकार के रूप में और (2) सगुण या निर्गुण भक्त कवियों की पुस्तकों में खण्डनों और प्रत्याख्यानों के विषय के रूप में।”
जिन सम्प्रदायों ने इस रहस्यात्मक साहित्य की सृष्टि की थी वे चिरकाल तक एक सुसंगठित सम्प्रदाय के रूप में नहीं रह सके, फलतः उनका साहित्य लुप्त हो गया। पूर्वी प्रदेशों में वह थोड़ा-बहुत इसीलिए सुरक्षित रह गया है कि 12वीं 13वीं शताब्दी तक वहाँ उक्त मत संगठित सम्प्रदाय के रूप में जीवित रहा। नेपाल आदि प्रदेशों से कुछ अल्प मात्रा में इस रहस्यात्मक साहित्य का उद्धार किया जा सका है।
उत्तर भारत का धर्म मत नवीन सम्पर्क और नवीन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बराबर अपनी पुरानी परम्परा पर कुछ अधिक दृढ़ता के साथ डटा रहा। हिमालय के पाददेश की साधना उसे अभिभूत नहीं कर सकी। यहाँ संस्कृत और ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा बहुत बाद तक बनी रही। इस प्रकार न तो हमें इस प्रदेश के ऐसे साहित्य का ही पता चलता है, जो राज-रक्षित हो और न ऐसे साहित्य का जो संगठित सम्प्रदाय द्वारा सुरक्षित हो। केवल जनता की जिह्वा पर जो कुछ बचा रहा, वही अनेक परिवर्तनों के बाद घट-बढ़कर क्वचित् कदाचित् मिल जाता है।
यह है आदिकाल के हिन्दी साहित्य के अरक्षित रहने की एक कल्पित मनोरंजक कहानी जो प्रायः श्रद्धेय आचार्य जी के शब्दों में उपन्यस्त की गई है।
अब प्रश्न यह उठता है कि चौदहवीं शताब्दी से पूर्व हिन्दी रचनाएँ उपलब्ध क्यों नहीं होतीं ? द्विवेदी जी इसके कुछ कारण-जैसे कि किसी सुदृढ़ सम्प्रदाय के संरक्षण का अभाव, शासक वर्ग की उपेक्षा तथा जन-मनोहर या लोकप्रिय साहित्य का अभाव आदि बताते हैं। इन कारणों में द्विवेदी जी के मतानुसार प्रधान कारण गहड़वार शासकों की हिन्दी के प्रति उपेक्षा भाव है। वे लिखते हैं- “इस प्रदेश की जनता से भिन्न और विशिष्ट बने रहने की प्रवृत्ति के कारण देशी भाषा और उसके साहित्य को आश्रय नहीं दे सके। अंतिम पीढ़ियों में ये लोग देशी भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने लगे थे।” समझ में नहीं आता है केवल गहड़वार नरेशों की उपेक्षा भाव से हिन्दी साहित्य क्यों नहीं पनप सका। हिन्दी सदा विरोधों और संघर्षों में पलती-जूझती आई है। वह अपनी अजस्र प्राणधारा और अदम्य शक्ति से विषम से विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर अपना मार्ग बनाती रही है। फिर उस समय क्या उसकी शक्ति कुंठित हो गई थी ? सच तो यह है कि चौदहवीं शताब्दी तक हिन्दी-साहित्य के प्रन्थों के उपलब्ध न होने के कारण कुछ और हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या गहड़वार नरेशों ने हिन्दी साहित्य की किसी रचना पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया था या उसे नष्ट करने की कोई आज्ञा निकाली थी ? फिर राज्याश्रय ही सब कुछ नहीं होता, धर्म और जनाश्रय भी उसे मिल सकता था। माना कि इस समय कोई सुसंगठित धार्मिक सम्प्रदाय नहीं था फिर भी एक-आध रचना तो अपने विशुद्ध रूप में सुरक्षित रह ही सकती थी और फिर इस विशाल देश का विराट जन-समूह एकाच रचना को भी अविकृत रूप में सुरक्षित नहीं रख सका ? संस्कृत साहित्य को अनेक बार विदेशी शासकों के निर्मम प्रहारों को सहना पड़ा फिर भी वह पूरी तरह विनष्ट नहीं हुआ जैसा कि अल्पकालीन शासकीय उपेक्षा से हिन्दी साहित्य ऐसा क्यों ? इसके अतिरिक्त डॉ० दशरथ शर्मा जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार भी द्विवेदी जी की उक्त मान्यता का खंडन करते हुए लिखते हैं- “कन्नौज सदा से देशी भाषा को मान देता रहा है। यदि संस्कत व संस्कृति के प्रबल समर्थक गोविन्दचन्द्र ने भी देश्य भाषा को इतना मान दिया तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि उसके दो पूर्वजों ने ही देशी भाषा का विरोध किया था और उन्होंने विरोध किया भी तो तीस-चालीस वर्षों में किसी भाषा का साहित्य सर्वथा नहीं हो जाता।” यह भी ध्यान रहे कि कन्नौज पर गहड़वारों का आधिपत्य 1090 ई० में हुआ था तथा देशी भाषा को आश्रय देने वाले गोविन्द चन्द्र सन् 1114 में गद्दी पर बैठे। इस पर द्विवेदी जी का उपेक्षित काल 24 वर्ष का ही ठहरता है। इस अल्पकालीन उपेक्षा के कारण पूर्ववर्ती शताब्दियों का साहित्य समूल नष्ट हो गया, यह तर्क कुछ अकल्पनीय लगता है।
इसके साथ-साथ एक और प्रश्न उठता है कि यदि उस काल का साहित्य उपलब्ध नहीं होता तो उन अज्ञात और आरक्षित रचनाओं के आधार पर इतिहास का ढांचा किस प्रकार खड़ा किया गया और उसका नामकरण कैसे सम्पन्न हुआ ? इस संबंध में डा० गणपति चन्द्र गुप्त के विचार अवलोकनीय हैं-“वस्तुतः इस युग में हिन्दी की प्रामाणिक रचनाएं न मिलने का कारण मुसलमानों का आक्रमण, देश की अशान्ति या किसी शासन विशेष की अवज्ञा नहीं है। यदि ऐसा होता तो इस युग में रचित अपभ्रंश की शताधिक रचनाएं उपलब्ध न होतीं। यह युग साहित्य की दृष्टि से अपभ्रंश का युग है किन्तु हम इसे बलात हिन्दी का आदिकाल या वीरगाथा काल सिद्ध करना चाहते हैं; फलस्वरूप कभी हम अपभ्रंश की रचनाओं को उधार ले लेते हैं, कभी अस्तित्वहीन या परवर्ती रचनाओं का आश्रय ग्रहण करते हैं और कभी साहित्य नष्ट हो जाने की मनगढ़ंत कहानियां कहकर आंसू बहाते हैं।” हम प्रस्तुत पुस्तक के “हिन्दी साहित्य के आदिकाल का नामकरण तथा पूर्वापर सीमानिर्धारण” नामक प्रकरण में बता चुके हैं कि हिन्दी भाषा का आरंभ लगभग 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया जा सकता है। उक्त मान्यता के आधार पर प्रन्याभाव की समस्या का सहज में ही समाधान हो जाता है। वस्तुतः वह युग अपभ्रंशों का युग था, स्वयं आचार्य हजारीप्रसाद के निम्नांकित शब्दों में यही तथ्य ध्वनित हो जाता है, ‘वस्तुतः 14वीं शताब्दी के पहले ही भाषा का रूप हिन्दी प्रदेशों में क्या और कैसा था, इसका निर्णय करने योग्य साहित्य आज उपलब्ध नहीं हो रहा है। जो एकाध शिलालेख और प्रन्थ मिलते हैं वे बताते हैं कि यद्यपि गद्य की और बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रचार बढ़ने लग गया था, पर पद्य में अपभ्रंश का ही प्राधान्य था। “
IMPORTANT LINK
- कबीरदास की भक्ति भावना
- कबीर की भाषा की मूल समस्याएँ
- कबीर दास का रहस्यवाद ( कवि के रूप में )
- कबीर के धार्मिक और सामाजिक सुधार सम्बन्धी विचार
- संत कबीर की उलटबांसियां क्या हैं? इसकी विवेचना कैसे करें?
- कबीर की समन्वयवादी विचारधारा पर प्रकाश डालिए।
- कबीर एक समाज सुधारक | kabir ek samaj sudharak in hindi
- पन्त की प्रसिद्ध कविता ‘नौका-विहार’ की विशेषताएँ
- ‘परिवर्तन’ कविता का वैशिष्ट (विशेषताएँ) निरूपित कीजिए।






