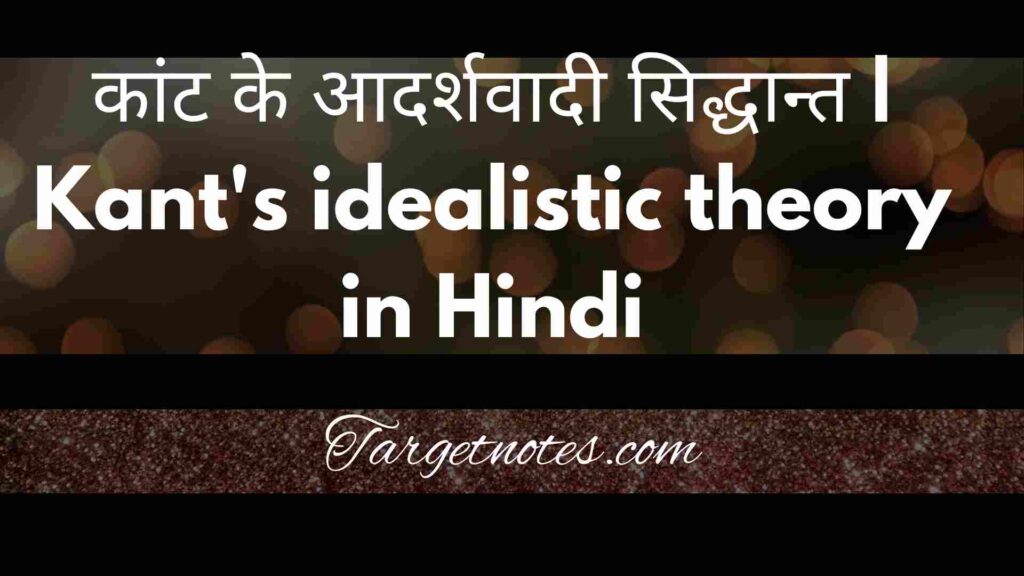
कांट के आदर्शवादी सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
आदर्शवाद की मूल संकल्पना तत्त्वमीमांसा के क्षेत्र से जुड़ी है जिसमें यह विचार करते हैं कि सृष्टि का सार-तत्त्व क्या है? आदर्शवाद के अंतर्गत ग्रह विश्वास किया जाता है कि इस जगत् में जिन भी वस्तुओं का अस्तित्व है, वे भौतिक वस्तुएँ नहीं हैं, बल्कि वे केवल मानसिक वस्तुएँ अर्थात् प्रत्यय या विचार-तत्त्व हैं। दूसरे शब्दों में, सृष्टि का मूल तत्त्व या सार तत्त्व जड़-पदार्थ नहीं, बल्कि चेतना है। अतः यह सिद्धान्त जड़वाद या भौतिकवाद या भौतिकवाद का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, भौतिक जगत् की तरह सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएँ भी प्रत्यर्यो की अभिव्यक्ति मात्र हैं। अत: इतिहास के किसी भी चरण में सामाजिक संस्थाओं में निहित प्रत्यय जितना उन्नत, उत्कृष्ट या उदात्त होगा, वह समाज उतना ही उन्नत और महान् हागा। इस तरह यह सिद्धान्त आदर्श की कल्पना से अनुप्राणित होकर ‘आदर्शवाद’ का रूप धारण कर लेता है।
आदर्शवाद के आरंभिक संकेत प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो (428-348) ई. पू.) के चिंतन में ढूंढ़े जा सकते हैं। आधुनिक राजनीति-चिंतन के अंतर्गत आदर्शवाद की चिंता का मुख्य विषय स्वतंत्रता का नैतिक आधार है। उदारवाद के अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए यह सोचा जाने लगा था कि मनुष्य का विवेक केवल अपने स्वार्थ का सही-सही हिसाब लगाने की क्षमता है। सामान्य हित की परिभाषा-भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के स्वार्थों के जोड़ के रूप में दी जा रही थी। यह प्रवृत्ति व्यक्ति को समुदाय से मुँह मोड़ने की प्रेरणा दे रही थी जिससे मनुष्य की नैतिक और सामाजिक भावना की बुनियाद खोखली हो रही थी। मानव-जीवन के इस अधूरेपन को भरना जरूरी था।
इन परिस्थितियों में जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट (1724-1804) ने 18वीं शताब्दी मैं मनुष्य की स्वतंत्रता के नैतिक आधार की ओर संकेत किया जिससे राजनीति- चिंतन में आदर्शवाद की ओर रुझान पैदा हुआ। 19वीं शताब्दी में जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल (1770-1831) ने इतिहास को चेतना की महान् यात्रा मानते हुए ऐसे समाज के उदय की आशा बँधाई जिसमें व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर विश्वजनीन परार्थवाद की भावना से प्रेरित होगे। फिर, अँग्रेज दार्शनिक टी. एच. ग्रीन (1836-82) ने कांट और हेगेल के आदर्शवाद को उदारवाद के साथ जोड़कर कल्याणकारी राज्य की शानदार पैरवी की। बर्नार्ड बोसांके (1848-1923) ने राज्य की सत्ता की नैतिक सीमाओं की ओर संकेत करके ग्रीन की परम्परा को आगे बढ़ाया।
कांट का आदर्शवाद- प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट (1724-1804) ने अपनी अनेक दार्शनिक कृतियों के माध्यम से दर्शनशास्त्र को समृद्ध किया जिसमें उसके राजनीतिक चिंतन की झलक भी मिलती है। इनमें ‘क्रिटीक ऑफ प्योर रीजन’ (शुद्ध तर्क मीमांसा, 1781), ‘ग्राउंडवर्क ऑफ मैटाफिजिक ऑफ मॉरल्स’ (नैतिक तत्त्वमीमांसा की आधारभूमि, 1785) और ‘ मैटाफिजिकल ऐलीमेंट्स ऑफ जस्टिस’ (न्याय के तात्विक मूलतत्व, 1797) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
‘ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र में अपने ‘अनुभवातीत आदर्शवाद’ का निरूपण करते हुए कांट यह तर्क दिया है कि सृष्टि के बारे में हमारा ज्ञान केवल ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त होने वाले गूढ़ और बिखरे हुए संकेतों पर आधारित है जिन्हें हमारा मन तर्कसंगत रूप में समन्वित करके सार्थक छाप लगी होती है। परन्तु यह सृष्टि अपने आप में क्या है, कैसी है इसका ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए सम्भव नहीं है। दूसरे शब्दों में, हम अपने अनुभव के आधार पर सृष्टि के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक ही उपाय रह जाता है कि हम अपने व्यावहारिक विवेक का सहारा लेकर ‘मन और ‘जगत्’ के परस्पर सम्बन्ध का पता लगा सकते हैं।
यह बात महत्त्वपूर्ण है कि हमारी सारी संकल्पनाएँ मानवीय गतिविधियों के सन्दर्भ में जन्म लेती हैं। ये गतिविधियाँ श्रम, विज्ञान और उन सब कलाओं के रूप में व्यक्त होती हैं जो विश्व को मानवीय उद्देश्यों और योजनाओं के अनुरूप ढालना चाहती हैं। अतः दर्शनशास्त्र के अंतर्गत यह पता लगाना चाहिए कि मनुष्य इस सृष्टि को मनचाहा रूप देने का प्रयास करते समय कौन-से तरीके अपनाते हैं? मनुष्य का व्यावहारिक विवेक भौतिक जगत् के कार्य-कारण सम्बन्ध के नियमों से नहीं बँधा है, बल्कि वह ‘ सद्-असद्’ अर्थात् भले-बुरे में अंतर करने में समर्थ है। अत: वह ‘नैतिक नियम’ से मार्गदर्शन प्राप्त करता है जो कि तत्त्वमीमांसा की बुनियाद है। इस तरह कांट ने ‘नैतिक नियम’ की प्रभुसत्ता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है जिसने आदर्शवादी दर्शन को विशेष रूप से आगे बढ़ाया है।
मानव-प्रकृति के सम्बन्ध में कांट के यही विचार मानव-गरिमा के सिद्धान्त की बुनियाद हैं। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते विशेष सम्मान का पात्र है, और किसी भी सांसारिक वस्तु के मूल्य से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते अपने-आप में साध्य है; वह किसी अन्य साध्य का साधन नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य को इस दृष्टि से देखने की सद्-इच्छा एक निरपेक्ष आदेश है, अर्थात् यह ऐसा नियम है जिसके साथ कोई शर्त नहीं जोड़ी जा सकती।
नैतिकता को सर्वोपरि स्थान देते हुए कांट ने यह विचार प्रकट किया है कि राजनीति को नैतिकता के सामने सदैव नतमस्तक रहना चाहिए। सच्ची राजनीति तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वह नैतिक आदर्शों का प्रणाम न कर ले। कांट के अनुसार नैतिकता की प्रेरणा ‘सद्-इच्छा’ से आती है, परन्तु राजनीति केवल कानूनी संस्थाओं का पुनर्निर्माण कर सकती है। यदि राजनीति को नैतिकता से जोड़ दिया जाए तो वह युद्ध पर प्रतिबंध लगाकर, शाश्वत शांति और मानव-अधिकारों पर बल देकर सार्वजनिक कानूनी न्याय की साधक बन सकती है।
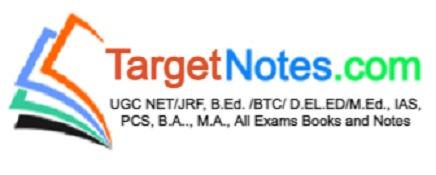




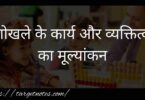

Thankyou so much Anjali for this great work