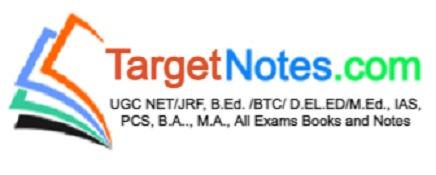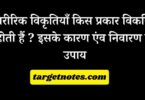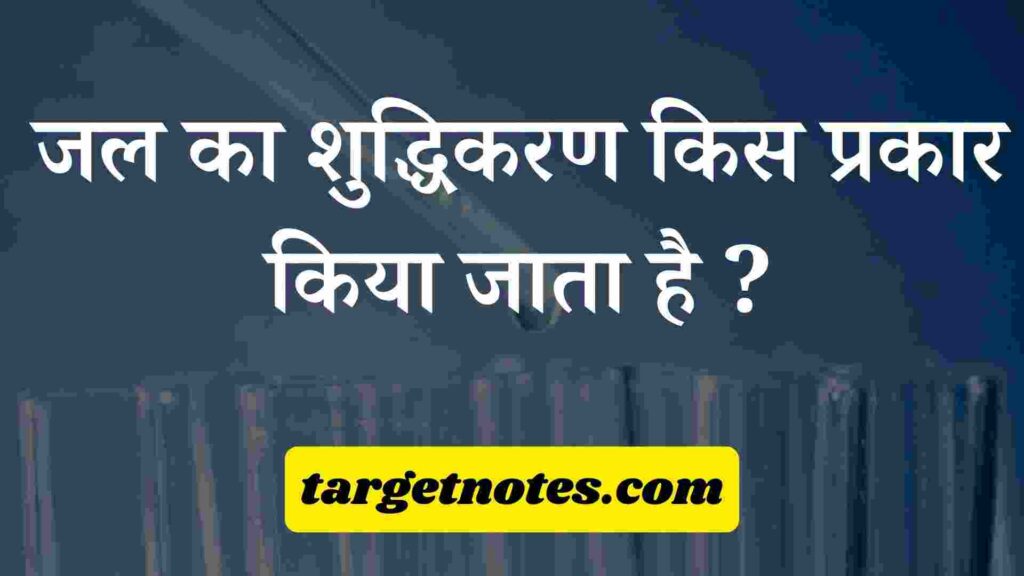
जल का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है ? वर्णन कीजिए। जल का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है ?
Contents
जल का शुद्धिकरण (Purification of Water)
पेयजल हमें विभिन्न प्रकार के साधनों से प्राप्त होता है। इसका शुद्ध होना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत जरूरी है। जल के शुद्धिकरण के दो प्रमुख साधन हैं – (1) प्राकृतिक एवं (II) कृत्रिम
(I) प्राकृतिक शुद्धिकरण (Natural Purification)-
प्राकृतिक शुद्धिकरण दो प्रकार का होता है-
- जल की वाष्प बनकर शुद्ध होना।
- नदी के जल में प्राकृतिक शुद्धता होना।
प्राकृतिक शुद्धता बनाये रखने के लिए विविध विधियाँ हैं-
(i) नदी में अनेक स्रोतों का जल बहकर आता है व मिल जाता है। अधिक जल मिल जाने (Dilution) से नदी के जल का शुद्धिकरण प्राकृतिक रूप से हो जाता है।
(ii) तलछट का बैठना (Sedimentation) इस प्राकृतिक विधि द्वारा नदी के जल में पाये जाने वाले दूषित तत्व स्वतः ही धीमी गति से नदी के जल में बैठते रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन तथा अन्य तत्त्वों के योग से भिन्न-भिन्न पदार्थों में ऑक्सीकरण तथा घटाव की क्रिया में मदद मिलती है और इसी तरह जल में पाये जाने वाले जीवाणुओं तथा गन्दगी में कमी आती है।
(iii) आकाश की वायुं और जल में विद्यमान ऑक्सीजन चेतनामुक्त पदार्थों (Organic matters) को तोड़-फोड़ कर सूक्ष्म और तरल बना देते हैं। इसी कारण जल में उपस्थित जीव-जन्तु इनका भक्षण कर जल शुद्ध करने में सहायता करते हैं।
(iv) प्रकाश की क्रिया से – आकृतिक रूप में सूर्य के प्रकाश में जो किरणें नदी के जल से पड़ती हैं, उनमें अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती है, जो जल में मौजूद जीवाणुओं को समाप्त करने में मदद करती हैं।
(v) अन्य विधि – नदी के जल में उपस्थित सहजीवी (Symbiotic) जीवाणु परजीवी जीवाणुओं को नष्ट करके जल का शुद्धिकरण करते रहते हैं।
(II) कृत्रिम साधन-
कृत्रिम साधन द्वारा भी जल का शुद्धिकरण किया जाता है। इनमें से प्रमुख-
- उबालना,
- वातन,
- निस्यन्दन तथा निष्क्रमण,
- आसवन तथा संघनन,
- अधिचूषण गन्ध एवं स्वाद से रिक्त करना,
- तलछठीकरण,
- लवणांश और जल की कठोरता दूर करना,
- स्कन्दन।
प्रायः जल का शुद्धिकरण दो स्तरों पर किया जाता है—
- सार्वजनिक जल वितरण के लिए बड़े पैमाने पर
- घरेलू उपयोग के लिये छोटे पैमाने पर।
यहाँ दोनों का विवरण दिया जा रहा है-
1. बड़े पैमाने पर जल का शोधन
प्रत्येक बड़े शहर में जल शोधन का कार्य वाटरवर्क्स द्वारा किया जाता है। इन वाटरवर्क्स द्वारा विभिन्न विधियाँ जल शोधन हेतु अपनाई जाती हैं; जैसे—(1) संग्रह, (2) निस्यन्दन, (3) क्लोरीनीकरण
1. संग्रह (Storage) – जल को प्राप्ति स्थान अर्थात् स्रोत से प्राप्त करने के उपरान्त उसको जलाशय में संग्रह कर लिया जाता है। इस कारण वह प्राप्ति स्थल पर होने वाले प्रदूषण से मुक्त रहता है तथा सामान्यतः 90% अशुद्धियाँ नीचे तली में बैठ जाती हैं। आमतौर पर जल को संग्रह करने के कारण कुछ रासायनिक और कुछ जैविक परिवर्तन भी आते हैं। जैसे नदी का पानी 10 से 15 दिन तक संग्रह के बाद रखा रहे तो हानिकारक जीवाणुओं की संख्या तो कम होने लगती है, किन्तु एलगी (Algae) आदि जीवों के पैदा होने से जल में बदबू आने लगती है।
2. निस्यन्दन (Filtration)- इस विधि से जल में उपस्थित जीवाणु 98% से 99% तक समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी नगर या क्षेत्र की जलापूर्ति किसी तालाब, झील या नदी पर निर्भर है तो उसके भौतिक, रासायनिक और जीवाणु सम्बन्धी सभी दोषों को नष्ट अवश्य कर दिया जाये। सामान्यतः इन दोषों को दूर करने के लिए फिल्टर को उपयोग में लाते हैं। निस्यन्दन मुख्यतः निम्न प्रकार के फिल्टरों से किया जाता है—
- धीमी गति फिल्टर (Slow Sand Filter),
- रैपिड मैविटी फिल्टर (Rapid Gravity Filter)
1. धीमी गति फिल्टर (Slow Sand Filter)- धीमी गति फिल्टर द्वारा फिल्टरेशन को अंग्रेजी प्रणाली भी कहा जाता है। इस फिल्टरेशन हेतु एक सैटलिंग टैंक, फिल्टर बैड तथा फिल्टर किये जल के लिए स्टोरेज टैंक व प्रयोगशाला की व्यवस्था होना आवश्यक है। सर्वप्रथम सैटलिंग टैंक (Settling Tank) में नदी, तालाब या झरने का जल संग्रह किया जाता है। लगभग 48 घण्टे तक इसमें रखने से जल में आलम्बित अशुद्धियाँ नीचे तल में बैठ जाती हैं। अगर जल में फिटकरी मिला दी जाए तो जल की अशुद्धियाँ शीघ्रता से बैठ जाती हैं। फिटकरी को कोग्लेट (Coagulat) कहा जाता है। फिटकरी के मिश्रण से जल का स्वाद बेहतर व दुर्गन्ध को कम किया जा सकता है। प्रायः वर्षा ऋतु के दौरान जीवाणु नष्ट करने के लिए जल में अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है
फिल्टर बैड- फिल्टर बैड के क्षेत्र को कई भागों में विभाजित किया जाता है। इस क्षेत्र को छानने वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रत्येक बैड विभिन्न आकार का मुँह बन्द (Water Tight) संग्रहणालय होता है। आमतौर पर यह अलग-अलग रेखाओं में एक साथ बराबर में बने होते हैं। सैटलिंग टैंक में संग्रहित जल को फिल्टर बैड (Filter-Bed) में धीरे-धीरे ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है। एक वर्ग फीट आकार का फिल्टर एक दिन में अनुमानतः 50 गैलन संग्रहितता जल का शुद्धिकरण करता है। फिल्टर बैड सदैव आयताकार होते हैं। इनकी गहराई आवश्यकता के अनुरूप 12 फीट से 15 फीट तक होती है। फिल्टर बैड से पाई जाने वाली सतहें निम्नवत् होती हैं-
- ऊपरी खाली स्थान – 2 से 3 फीट तक
- जल की गहराई – 5 से 6 फीट तक
- बारीक बालू (Fine crushed Sand) – 1 से 3 फीट तक
- मोटी बालू (Coarse Sand) – 1/2 से 1 फीट तक
- कंकड़ – 1/2 से 1 फीट तक
- ईंट (Brick)- दो तह
इन सतहों की मोटाई भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती है। छने हुए जल को ईंटों की नालियों व धाराओं में व्यवस्थित कर निष्कासित किया जाता है। निरन्तर व एक गति का निस्यन्दन स्थिर करने के लिए फिल्टर बैडों में वाल्व (Valve) लगे होते हैं। इनमें कुछ आन्तरिक व कुछ बाह्य तत्त्व होते हैं।
फिल्टर की क्रिया-
स्लोसैण्ड फिल्टर निम्न प्रकार से क्रिया करता है-
(क) भौतिक कार्य- फिल्टर बैड की ऊपर सतह पर ही आलम्बित अशुद्धियों को पृथक् कर रोका जाता है, परन्तु फिर भी कुछ जीवाणु कंकड़ पत्थरों की सतह पार कर जाते हैं व आमतौर पर 99% तक जीवाणु ऊपर सतह पर फिल्टर हो जाते हैं।
(ख) रासायनिक क्रिया- इस कार्य के द्वारा वायु की उपस्थिति में जल के कार्बनिक तत्त्वों का नाइट्रीकरण और ऑक्सीकरण जीवाणु की मदद से होता है।
(ग) जैविक सतह (Vital layer)- में जीवाणु सम्बन्धी वास्तविक कार्य-फिल्टर बैड के 2-3 दिन तक कार्य करने के बाद कई निम्न श्रेणी के वानस्पतिक पदार्थ जैसे एलगी (Algas), कवक (Fungi) एकत्रित होकर एक सब्ज परत बना लेते हैं, जिसे जैविक सतह (Vital layer) कहा जाता है। यह सतह बालू के ऊपर जमती है। यह सतह जल में उपस्थित जीवाणुओं को जमा करती है। इस जमाव की सतह मोटी होती जाती व निस्यन्दन की गति धीमी होती जाती है। ऐसी स्थिति में 1 इंच तक सतह को काटकर छील दिया जाता है। निस्यन्दन के पश्चात् जल में क्लोरीन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। प्रति सप्ताह जल (निस्यन्दित जल) का प्रयोगशाला में जीवाणु परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए।
इस फिल्टर के निर्माण में व्यय अधिक आता है, साथ ही अधिक बड़े स्थान की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु धीमी गति से फिल्टरेशन के कारण घने जल की 99% जीवाणु व अशुद्धियों से मुक्ति हो जाती है। कभी-कभी क्लोरीनीकरण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती।
2. रैपिड ग्रैविटी फिल्टरेशन (Rapid Gravity Filtration)- इस विधि को अमेरिकन विधि भी कहा जाता है। इसको रैपिड कहने का तात्पर्य इसकी निस्यन्दन शक्ति की तीव्रता बताते हैं। इसकी निस्यन्दन शक्ति स्लोसैन्ड फिल्टर की तुलना में 40 से 60 गुना अधिक होती है। इसके प्रयोग व निर्माण में व्यय कम, प्रयोग में सरल व सुगम होता है। इसके लिए स्लोसैण्ड फिल्टर की तुलना में कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। यह फिल्टर विशेषतः यान्त्रिक निस्यन्दन की क्रिया पर आधारित होता है व प्रतिदिन लगभग 130 गैलन प्रतिवर्ग फुट तक फिल्टरेशन में समर्थ होता है।
सामान्यतः इस फिल्टर में लकड़ी, लोहे या कंकरीट (RCC) के 7 फीट गहरे सिलेण्डर होते हैं, जिनमें जल को बालू की सतहों द्वारा छाना जाता है। इसमें ऊपर की बालू की सतह की मोटाई 27 से 36 इंच तक तथा निचली सतह (कंकड़ वाली) की मोटाई 12 से 18 इंच तक होती है। इसमें दो प्रकार के फिल्टर होते हैं-1. दबावी फिल्टर, 2. प्रैविटी फिल्टर। दबावी फिल्टर का चैम्बर सदैव बन्द रहता है और कोगूलैण्ट किया जल वाल्व द्वारा खींचा जाता है।
रैपिड ग्रैविटी फिल्टरेशन दो क्रियाओं पर प्रमुखतः आधारित होता है-
- स्कन्दन (Coagulation)
- झाग निर्माण (Formation of Floc)
- निस्यन्दन (Filteration)
इस प्रणाली के अन्तर्गत स्लोसैण्ड फिल्टर वाली जैविक सतह का स्थान कृत्रिम रूप से निर्मित निस्यन्दन परत को दिया जाता है। यह निस्यन्दन परत घनीभूत तलछट तैयार कर निर्मित की जाती है।
रैपिड प्रैविटी फिल्टर कई प्रकार के होते हैं, किन्तु प्रमुख रूप से पैटरसन का रैपिड फिल्टर सर्वोत्तम व सुगम है। इस विधि में संग्रहित जल को चार विशेष क्रियाओं द्वारा तीव्रता से छाना जाता है। ये क्रियाएँ निम्नलिखित हैं-
(अ) स्कन्दन (Coagulation) – इस प्रक्रिया में नदी या ताल का जल एक सैटलिंग टैंक में पाइपों की सहायता से पहुँचा दिया जाता है। इस सैटलिंग टैंक यह जल लगातार प्लाण्ट में जाता रहता है। तत्पश्चात् इसमें फिटकरी अथवा एलम सल्फेट (Alum Sulphate) अर्थात् कोगूलैण्ट को 1 से 4 मैन प्रति गैलन के अनुपात में मिलाया जाता है, जो नीचे की ओर बहता है तथा कुण्ड में बैफल प्लेटों (Baffle Plates) की सहायता से पहुँचकर पूर्णतः जल में विलीन हो जाता है।
(व) तलछटीकरण (Sedimentation) – जल का कुण्ड में प्रवेश के उपरान्त जल में उपस्थित आलम्बित पदार्थ या तत्त्व तल में जमा हो जाते हैं। इस कुण्ड में जल को 3 से 6 घण्टे तक रखा जाता है।
(स) निस्यन्दन (Filtration)- तलछटीकरण क्रिया के उपरान्त जल को तीव्र फिल्टरों की श्रृंखला में भेजा जाता है। जल में घुलित कोगूलैण्ट बालू की सतह पर जीवाणु व शैवाल (Algae) की मदद से एक वैतन्य जैविक सतह (Vital layer) को निर्मित करता है, जिससे जल को इसके ऊपर से गुजारा जाता है।
(द) क्लोरीनीकरण (Chlorination) – फिल्टेरशन के पश्चात् प्राप्त जल को स्वचलित गीयर से होकर क्लोरीनिंग टैंक में प्रवेश कराया जाता है। इस क्लोरीनिंग टैंक में जल में क्लोरीन गैस को मिलाकर जल विसंक्रमित किया जाता है। जिससे सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।
रैपिड ग्रैविटी फिल्टर के लाभ-
इसके निम्नवत् अनेक लाभ होते हैं-
- ये फिल्टर सीधे ही प्राप्त जल पर कार्य कर सकते हैं व संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती।
- ये स्थान कम घेरते हैं।
- इसमें जल का द्धिकरण तीव्रता से होता है।
- इससे वैकवाशिंग (परवधोवन) सरलता से हो जाता है। इसमें 95% जल कीटाणु रहित हो पाता है। इससे क्लोरीनीकरण करना आवश्यक हो जाता है।
स्लो सैण्ड और रैपिड ग्रेविटी फिल्टरेशन की तुलना
| स्लोसैण्ड फिल्टरेशन | रैपिड प्रैविटी फिल्टरेशन |
| 1. यह अंग्रेजी विधि है। | 1. यह अमेरिकन विधि है। |
| 2. यह एक प्राचीन प्रणाली है। | 2. यह आधुनिक प्रणाली है। |
| 3. इसके लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। | 3. इसके लिए कम भूमि की आवश्यकता होती है। |
| 4. इसके निर्माण में व्यय अधिक होता है, किन्तु इसकी प्रणाली चालू रखने में खर्च कम पड़ता है। | 4. इसके निर्माण में कम व्यय होता है, किन्तु इसकी प्रणाली चालू रखने में अधिक खर्च पड़ता है। |
| 5. इसमें कोगूलैण्ट की आवश्यकता नहीं होती। | 5. इसमें कोगूलैण्ट की आवश्यकता होती है। |
| 6. यह विधि साफ या हल्के गन्दे जल के लिए उपयुक्त है। | 6. यह विधि गन्दे जल के लिए उपयुक्त है। |
| 7. इसमें सैटलिग टैंक की व्यवस्था करना आवश्यक है। | 7. इसमें सैटलिंग टैंक की व्यवस्था करना अनिवार्य नहीं है। |
| 8. इसमें शैवाल की वृद्धि निस्यन्दन क्रिया को अवरुद्ध करती है। | 8. इसमें शैवाल की वृद्धि नहीं होती है। |
| 9. फिल्टर बैड के माध्यम से जल धीमी गति से छनता है। | 9. इनमें जल तेज गति से छनता है। |
| 10. इसमें परिणाम समान तथा अच्छे रहते हैं, इसलिए जल के क्लोरीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। | 10. इसमें परिणाम समान तथा अच्छे नहीं रहते, इसलिए जल को क्लोरीन से विसंक्रमित या जीवाणुरहित बनाना अनिवार्य है। |
| 11. इसकी साधारण दर प्रति एकड़ प्रतिदिन 25 लाख से 40 लाख गैलन है। यह रैपिड फिल्टरेशन से 40 से 60 गुना कम होती है। | 11. इसके द्वारा प्रति एकड़ प्रतिदिन 100 से 200 लाख गैलन जल प्रदान किया जाता है। |
| 12. इसकी सफाई बालू की ऊपरी सतह को छीलने से होती है। | 12. यह जल की विपरीत धारा के द्वारा साफ किया जाता है। कभी-कभी बालू को यान्त्रिक ढंग से हवा के दबाव से ढीला किया जाता है इसलिए इसको मैकेनिकल फिल्टर भी कहा जाता है। |
| 13. इसमें जल को धीरे-धीरे बड़े छिछले बन्द संग्रहालय में बालू की सतह से होकर गुजरना पड़ता है। | 13. इसमें जल तीव्र गति से लकड़ी, लोहे या कंकरीट की हौदों में रखी हुई बालू से गुजरता है। इसमें मोटी बालू का प्रयोग किया जाता है। |
| 14. इसमें भौतिक, रासायनिक तथा जीवाणु सम्बन्धी विशुद्धियाँ रहती हैं। इसकी प्रक्रिया समान रहती है। | 14. इसकी कार्य प्रणाली मुख्यतः यांत्रिक है। इससे दूषित, कीचड़ तथा रंगयुक्त जल शुद्ध किया जाता है। इसको प्रक्रिया असमान रहती है। |
क्लोरीनीकरण प्रक्रिया – सामान्यतः जल को शुद्ध करने की यह एक अनुपूरक क्रिया है। इसमें निस्यन्दकों द्वारा प्रदत्त जल को स्वच्छ व निर्मल बनाने हेतु क्लोरीनीकृत किया जाता है। क्लोरीन द्वारा हानिप्रद जीवाणुओं का सफाया हो जाता हैं। व साथ ही साथ जल का स्वाद बेहतर व दुर्गन्ध समाप्त हो जाती है।
इस क्रिया में क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है तथा इसके मिश्रण से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व हायपोक्लोरस अम्ल सारे जल को शुद्ध करते हैं।
क्लोरीन को जल में मिलाने हेतु इसके लिए विशेष निर्मित पम्प की सहायता ली जाती है। क्लोरीन गैस आँखों में जलन उत्पन्न करती है व विषाक्त होती हैं। इसके दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर अब वृहद स्तर पर ओजोन गैस का प्रयोग किया जाने लगा है। ओजोन गैस भी शक्तिशाली ऑक्सीकरण करती है, जिससे पानी का स्वाद, दुर्गन्ध, रंग आसानी से परिवर्तित हो जाता है।
(2) छोटे पैमाने पर जलशोधन
प्रायः हमारे देश में घरेलू उपयोग हेतु जल शुद्धिकरण निम्नलिखित तीन प्रकार से किया जाता है:-
- उबालकर या आसवन द्वारा,
- रासायनिक निष्संक्रमण द्वारा,
- निस्यन्दन द्वारा।
1. जल को उबालना (Boiling of Water)-
हमारे देश में जिन क्षेत्रों में नदी या तालाब का जल सीधे ही उपयोग में लाया जाता है, वहाँ पहले जल को उबाला जाता है। इस क्रिया में लाये गये जल को 20 मिनट तक लगातार अच्छी तरह उबालकर ठण्डा कर लिया जाता है। इससे जल में उपस्थित जीवाणु व अशुद्धियाँ दूर हो जाती है तथा जल की कठोरता भी नष्ट हो जाती है। ठण्डा करने के पश्चात् प्रयोग करने हेतु बर्तनों में छानकर एकत्रित कर लिया जाता है। इससे जल का स्वाद, दुर्गन्ध व रंग परिवर्तित हो जाता है। यह स्वादरहित हो जाता है। उबाले हुए जल को वायुयुक्त करना आवश्यक है।
आसवन (Distillation) – इस क्रिया में जल को उबालकर वाष्प बनायी जाती है व फिर वाष्प को ठण्डा करके जल में परिवर्तित कर ली जाती है। इस जल को आसुत जल कहा जायेगा। यह जल स्वादहीन होता है। स्वादिष्ट बनाने के लिए जल को वायुयुक्त कर लेना चाहिए। समुद्र का खारा जल इसी विधि से पीने योग्य बनाया जाता है। समुद्री जहाजों पर प्रायः यही जल पीने के काम आता है।
2. रासायनिक निष्संक्रमण द्वारा (Chemical Process) –
पेयजल को शुद्ध करने के लिए दो रासायनिक पदार्थ मिलाये जाते हैं—
- अवक्षेपक,
- जीवाणुनाशक।
1. अवक्षेपक (Precipitant) –
इससे जल की अशुद्धियाँ अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाती हैं, किन्तु नष्ट नहीं हो पाती हैं।
अवक्षेपकों का प्रकार
(अ) फिटकरी (Alum) – जल में उपस्थित कैल्सियम कार्बोनेट पर फिटकरी की क्रिया होती है, जिसके कारण जल की अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इससे जीवाणुओं का नाश नहीं होता व कुछ संख्याओं में कमी अवश्य आती है। एक प्रयोग के अनुसार, 5 लीटर अशुद्ध जल में आधा ग्राम फिटकरी मिलने से अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं व तत्पश्चात् 300 मिलीग्राम चूना मिला देने से जल अत्यन्त स्वच्छ हो जाता है।
(ब) निर्मली – निर्मली एक वृक्ष का फल है। बर्तन को जल से भरने से पहले निर्मली के बर्तन की अन्दरूनी सतहों पर रगड़ लेते हैं। इसके बाद बर्तन में जल भर देते हैं। कुछ देर पश्चात् जल में उपस्थित सभी अशुद्धियाँ तली में जम जाती हैं। हमारे देश के कई क्षेत्रों में इस विधि का प्रयोग होता है।
2. जीवाणुनाशक (Germicides) –
जीवाणुनाशक द्वारा जल में उपस्थित जीवाणु और अन्य ऐन्द्रिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं।
जीवाणुनाशक का प्रयोग
जल के शुद्धिकरण के लिए कई जीवाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है|
(A) पोटेशियम परमैगनेट (Potassium Permanganate KMNO4 ) – जल को शुद्ध करने हेतु सर्वोत्तम जीवाणुनाशक पोटेशियम परमैगनेट ही है। यह एक रासायनिक पदार्थ है। वर्षा के दिनों में तालाब तथा कुएँ का जल अशुद्ध हो जाता है तो पोटेशियम परमैगनेट का प्रयोग सर्वाधिक रूप से किया जाता है। प्रायः इसके प्रयोग की मात्रा लगभग 200 गैलन जल में ग्राम मिला देने से पूरा जल शुद्ध हो जाता है। हैजे के जीवाणुओं पर यह विशेष प्रभावी है।
(B) आयोडीन (Iodine) – जल के 2000 भाग में अगर भाग शुद्ध आयोडीन का मिला दिया जाये तो मात्र 10 मिनट में जल जीवाणुरहित हो जाता है। ऐसा प्रयोगों से निष्कर्ष मिला है। आयोडाइड ,आयोडेट ऑफ सोडा की 150 मिप्रा० की एक टिकिया एवं इतनी ही मात्रा में एसिड की मिलाकर यदि 20 लीटर जल में डालने से मोतीझरा व हैजे के जीवाणु बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं।
(C) नीला तृतिया (Copper Sulphate)- कुएँ, तालाब तथा बड़े-बड़े संग्रह केन्द्रों पर इसका प्रयोग किया जाता है, किन्तु अब इसका प्रयोग प्रचलन में नहीं, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्रयोग होता है अन्यथा नहीं।
(D) ओजोन (Ozone) – जल का शुद्धिकरण ओजोन द्वारा भी होता है। सर्वप्रथम बिजली के प्रयोग से वायु को ओजोनीकृत किया जाता है। तत्पश्चात् जल को वायु का सम्पर्क कराया जाता है, जिससे जल में उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं।
(E) ब्लीचिंग पाउडर (Bleaching Powder)- यह सफेद रंग का पाउडर है, जो अत्यन्त सस्ता व सरलता से सर्वत्र उपलब्ध होता है। इसको बनाने के लिए क्लोरीन गैस को चूने से मिलाया जाता है। इसका प्रयोग कुओं का जल शुद्ध करने में प्रमुख रूप से किया जाता है।
(F) चूना- कुछ जगह ताजे चूने से भी जल को शुद्ध करने का तरीका अपनाया जाता है, किन्तु पुराने चूने में शोधन की कोई शक्ति या क्षमता नहीं होती है।
(G) क्लोरीन (Chlorine) – क्लोरीन का प्रमुखता से प्रयोग शहरों के वाटर वर्क्स विभाग द्वारा किया जाता है। दस लाख भाग जल में एक भाग क्लोरीन की मात्रा पर्याप्त होती है।
3. निस्यन्दन (Filteration)-
घरेलू स्तर पर जल के निस्यन्दन हेतु निम्न फिल्टर प्रयोग में लाये जाते हैं-
(अ) जियोलाइट फिल्टर- वर्तमान में अशुद्ध जल को शुद्ध व स्वाद वाला बनाने के लिए जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। जियोलाइट लकड़ी के बुरादे की भाँति एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, जिसके कारण जल में विद्यमान मैग्नीशियम और कैल्सियम का ग्रहण होता है तथा सोडियम का परित्याग होता है। प्राकृतिक रूप में प्राप्त होने वाला जियोलाइट को हरी बालू (Green Sand) या ग्लूकोनाइट (Gluconite) कहते हैं। सोडियम सिलिकेट युक्त संश्लेषित जियोलाइट को परम्यूटिट कहते हैं।
कैल्सियम तथा मैग्नीशियम युक्त जल में परम्यूटिट मिलाने से जियोलाइट में उपस्थित सोडियम जल में मिल जाता है तथा अन्य लवणों को एक मिट्टी सोख लेती है। इस प्रकार के प्रयोग को बेस एक्सचेन्ज विधि (Base Exchange Method) भी कहा जाता है।
(ब) पाश्चर चेम्वरलेन फिल्टर (Pasteur-Chamberlain Filter)- इसमें चीनी मिट्टी से निर्मित खोखली नलो जिसमें एक छिद्र होता है एक बर्तन में जमाकर रख दी जाती है। यह बर्तन एक नल से जुड़ा होता है। नल से आने वाला जल चीनी मिट्टी की नली के छिद्र में से जोर से खोखले भाग में आता है। खोखली नली के छिद्र अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं। जिसके कारण अशुद्ध पदार्थ और अत्यन्त सूक्ष्म कीटाणु नहीं निकल पाते हैं तथा दूसरी ओर नली को समय-समय पर उबलते हुए जल में रखना पड़ता है और बाहरी बार्डर को ब्रश से साफ करना पड़ता है।
(स) वर्गफील्ड फिल्टर–वर्गफील्ड फिल्टर में लगा सिलेण्डर इन्फ्यूसोरियल मिट्टी का निर्मित होता है। इसकी विशेषता है कि यह जल को तीव्र गति से छानता है। साथ ही साथ इसके लिए किसी भी दबाव की आवश्यकता नहीं होती। मिट्टी के सिलेण्डर को 2-3 दिन के अन्दर गर्म जल से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।
IMPORTANT LINK
- नवजात शिशु की क्या विशेषताएँ हैं ?
- बाल-अपराध से आप क्या समझते हो ? इसके कारण एंव प्रकार
- बालक के जीवन में खेलों का क्या महत्त्व है ?
- खेल क्या है ? खेल तथा कार्य में क्या अन्तर है ?
- शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य | Mental Health of Teachers in Hindi
- मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या सम्बन्ध है?
- मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एंव लक्षण
- खेलों के कितने प्रकार हैं? वर्णन कीजिए।
- शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में खेल एंव खेल के सिद्धान्त
- रुचियों से क्या अभिप्राय है? रुचियों का विकास किस प्रकार होता है?
- बालक के व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- चरित्र निर्माण में शिक्षा का क्या योगदान है ?
- बाल्यावस्था की प्रमुख रुचियाँ | major childhood interests in Hindi
- अध्यापक में असंतोष पैदा करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं?
Disclaimer