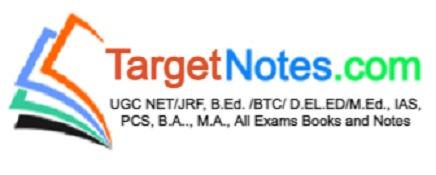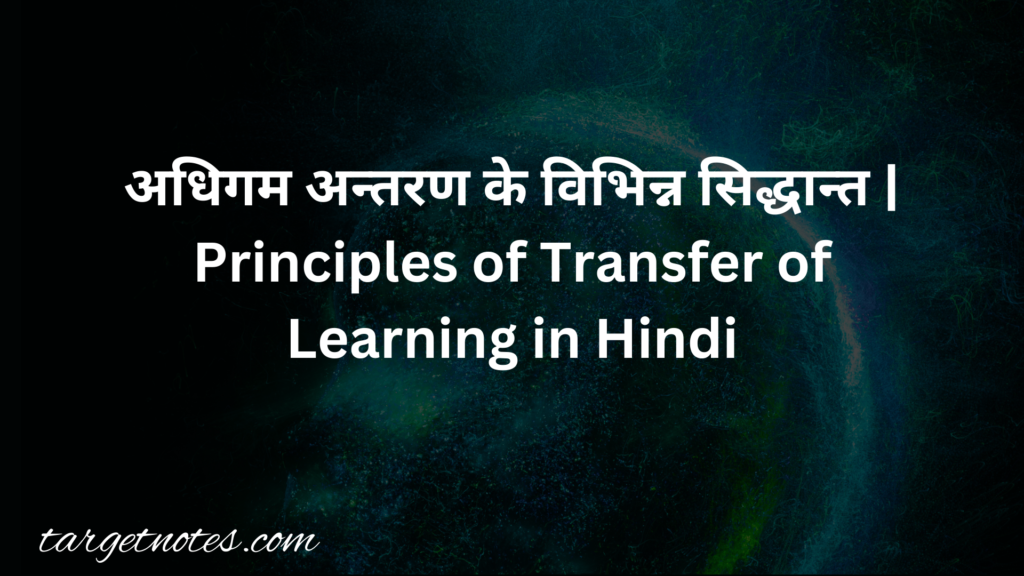
अधिगम अन्तरण के विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।
सीखने के अन्तरण के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों की रुचि अत्यंत प्रारम्भ से ही रही है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अन्तरण से सम्बन्धित अनेक प्रयोग करके अन्तरण के अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने में सफलता पाई है। पाठकों के अवबोध के लिए अधिगम अन्तरण (Transfer of learning) के सभी सिद्धान्तों की संक्षिप्त चर्चा आगे की जा रही है।
1. मानसिक अनुशासन का सिद्धान्त (Theory of Mental Discipline) – मानसिक अनुशासन का सिद्धान्त अन्तरण का अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तरण स्वतः होता है। अन्तरण के लिए केवल मानसिक क्रियाओं का विकास एवं अभ्यास होना चाहिए। जैसे यदि तर्क शक्ति का विकास हो गया है तो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकेगा तथा यदि निरीक्षण शक्ति का विकास हो गया है तो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकेगा। अभ्यास के द्वारा विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। सीखने की सामग्री या विषयवस्तु के कठिन होने पर तथा उसका अधिक अभ्यास करने पर मानसिक शक्तियों का विकास अधिक होता है। लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, गणित जैसे विषयों को मानसिक शक्तियों के विकास की दृष्टि से अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार मानसिक शक्तियों के विकसित हो जाने पर व्यक्ति में एक मानसिक कार्य प्रणाली बन जाती है जो सभी परिस्थितियों में सीखने में सहायक होती है।
परन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते हैं। विलियम जेम्स (William James) ने सन् 1890 में सर्वप्रथम इस सिद्धान्त का खंडन किया। उसने स्मृति योग्यता के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रयोग किया। विलियम जेम्स ने विक्टर हृयूगो द्वारा रचित ‘सैटायर’ (Satyr) नामक काव्य की 158 पंक्तियों को याद किया जिसमें उसे 32 मिनट का समय लगा। फिर उसने मिल्टन के ‘पैराडाइज लास्ट’ नामक काव्य को अड़ती दिन तक 20 मिनट प्रतिदिन याद करने का अभ्यास किया। तत्पश्चात उसने विक्टर ह्यूगो के ‘सैटायर’ (Satyr) की अन्य 158 पंक्तियों को याद किया। इस बार उसे 52 मिनट का समय लगा। इस प्रकार से विलियम जेम्स ने देखा कि स्मरण करने के अभ्यास में स्मरण करने की योग्यता में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है।
थार्नडाइक (Thorndike) ने भी सन् 1924 में अपने अध्ययन में पाया कि लैटिन या फ्रेंच सीखने वाले छात्र शरीर विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों से अधिक योग्य नहीं थे। वेजमैन ने भी सन् 1945 में निष्कर्ष निकाला कि सीखने के स्थानान्तरण पर पाठ्य विषयों की उत्कृष्टता (Superiority) का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। .
2. समान अवयव का सिद्धान्त (Theory of Identical Elements) – समान अवयवों के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन थार्नडाइक (Thorndike) ने किया था। वस्तुतः समान अवयवों का सिद्धान्त थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सादृश्यता के नियम (Law of Analogy) का ही एक विस्तार (Extension) है। इस सिद्धान्त के अनुसार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अन्तरण उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में दोनों स्थितियों की विषयवस्तु, दृष्टिकोण, विधि, उद्देश्य आदि बातें समान होती हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सीखने का अन्तरण उस सीमा तक हो सकता है जिस सीमा तक सीखने की दोनों क्रियाओं में समानता होती है। यदि दोनों क्रियाओं में समानता अधिक होती है तो अन्तरण भी अधिक होता है। यदि समानता कम ‘होती है तो अन्तरण भी कम होता है। दो कार्यों, विषयों अथवा अनुभवों में जितनी अधिक समानता होती है, उतना ही अधिक वे एक दूसरे के अध्ययन में सहायक होते हैं। स्पष्ट है कि अन्तरण की प्रक्रिया में विषयवस्तु (Matter) तथा विधि (Method) नामक दो कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन दोनों की समानता अथवा असमानता ही अन्तरण की मात्रा को निर्धारित करती है। इस सिद्धान्त के अनुसार पियानो बजाने के प्रशिक्षण का लाभ टंकण (Type) करने में, कार चलाने का ज्ञान ट्रक चलाने में, साईकिल चलाने का ज्ञान स्कूटर चलाने में, संस्कृत पढ़ने का ज्ञान हिन्दी पढ़ने में, गणित सम्बन्धी ज्ञान भौतिक शास्त्र पढ़ने में, भूगोल सम्बन्धी ज्ञान इतिहास पढ़ने में सहायक होता है क्योंकि इनमें परस्पर काफी समानता होती है।
3. सामान्यीकरण का सिद्धान्त (Theory of Generalization) – सामान्यीकरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन सन् 1908 में सी.एच. जुड (C.H. Judd) ने किया था। जुड के अनुसार सीखने का अन्तरण वास्तव में छात्रों के द्वारा कुछ सामान्यीकृत सिद्धान्तों के निर्माण के फलस्वरूप होता है। छात्र अपने ज्ञान तथा अनुभवों के आधार पर कुछ सामान्य नियम या सिद्धान्त बना लेते हैं तथा इनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में करते हैं। किसी एक परिस्थिति में सीखे अथवा विकसित किये गये सिद्धान्तों के ज्ञान अथवा बोध का उपयोग छात्र अन्य परिस्थितियों में तभी कर सकते हैं जब दोनों परिस्थितियों में कुछ समानता होती है।
जुड ने एक प्रयोग किया। उसने छात्रों के दो समूहों को पानी में डूबी किसी वस्तु पर निशाना लगाने का अभ्यास कराया। तत्पश्चात् उसने एक समूह को अपवर्तन के नियमों का प्रशिक्षण दिया, परन्तु दूसरे समूह को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। अब अंत में उसने पानी में डूबी वस्तु की गहराई को परिवर्तित करके उस पर निशाना लगाने का परीक्षण लिया। उसने देखा कि जिस समूह को अपवर्तन के नियमों का प्रशिक्षण दिया था, उसके निशाने अधिक सही थे। जुड ने इस परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा कि अपवर्तन संबंधी नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त समूह इसलिए निशानों को सही लगाने में अधिक श्रेष्ठ था क्योंकि उसने अपवर्तन के सिद्धान्तों का अन्तरण नवीन परिस्थितियों में कर लिया था।
4. आरोपण का सिद्धान्त (Theory of Transposition) – अन्तरण के आरोपण के सिद्धान्त का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब एक गेस्टाल्ट दूसरे गेस्टाल्ट पर आरोपित हो जाता है तभी अन्तरण होता है। अन्तरण के इस सिद्धान्त के अनुसार एक परिस्थिति में अर्जित अन्तर्दष्टि अथवा सूझ का उपयोग व्यक्ति दूसरी परिस्थितियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए करता है।
5. सीखना सीखने का सिद्धान्त (Theory of learning to learn) – इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्यों को करते-करते उस प्रकार के कार्यों को करना सीख लेता है। जैसे कोई मोटर मैकेनिक नए प्रकार के इंजन को भी सरलता से समझ लेता है अथवा घड़ीसाज नई तकनीक पर आधारित घड़ी को खोलना सरलता से सीख लेता या गणित में एक प्रकार की समस्याओं को हल करने में कुशल छात्र गणित की दूसरे प्रकार की समस्याओ को हल करना सरलता से सीख जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अथवा छात्र ने उस प्रकार के कार्यों को करने की विधि को सीख लिया है।
इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिए वार्ड ने सन् 1937 में एक अध्ययन किया। उसने निरर्थक शब्दों की सूचियाँ बनाईं। प्रत्येक सूची में बारह शब्द थे तथा कठिनाई की दृष्टि से विभिन्न सूचियाँ समान रूप से कठिन थीं। छात्रों को एक दिन में एक सूची याद करने के लिए कहा गया। पहली सूची को याद करने के लिए छात्रों ने 38 बार दोहराया, जबकि सातवीं सूची को याद करने के लिए छात्रों ने 20 बार ही दोहराया तथा 16वीं सूची को छात्रों ने मात्र 14 बार दोहराया। स्पष्ट है कि छात्रों ने शब्दों को याद करने का तरीका सीख लिया था जिसके परिणामस्वरूप बाद की सूचियों को याद करने में उन्हें अपेक्षाकृत कम समय लगा।
Important Link…
- अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार के सिद्धान्त (स्रोत)
- अधिकार की सीमाएँ | Limitations of Authority in Hindi
- भारार्पण के तत्व अथवा प्रक्रिया | Elements or Process of Delegation in Hindi
- संगठन संरचना से आप क्या समझते है ? संगठन संरचना के तत्व एंव इसके सिद्धान्त
- संगठन प्रक्रिया के आवश्यक कदम | Essential steps of an organization process in Hindi
- रेखा और कर्मचारी तथा क्रियात्मक संगठन में अन्तर | Difference between Line & Staff and Working Organization in Hindi
- संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले संयोगिक घटक | contingency factors affecting organization structure in Hindi
- रेखा व कर्मचारी संगठन से आपका क्या आशय है? इसके गुण-दोष
- क्रियात्मक संगठन से आप क्या समझते हैं? What do you mean by Functional Organization?