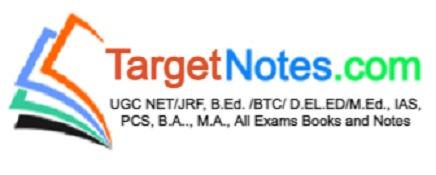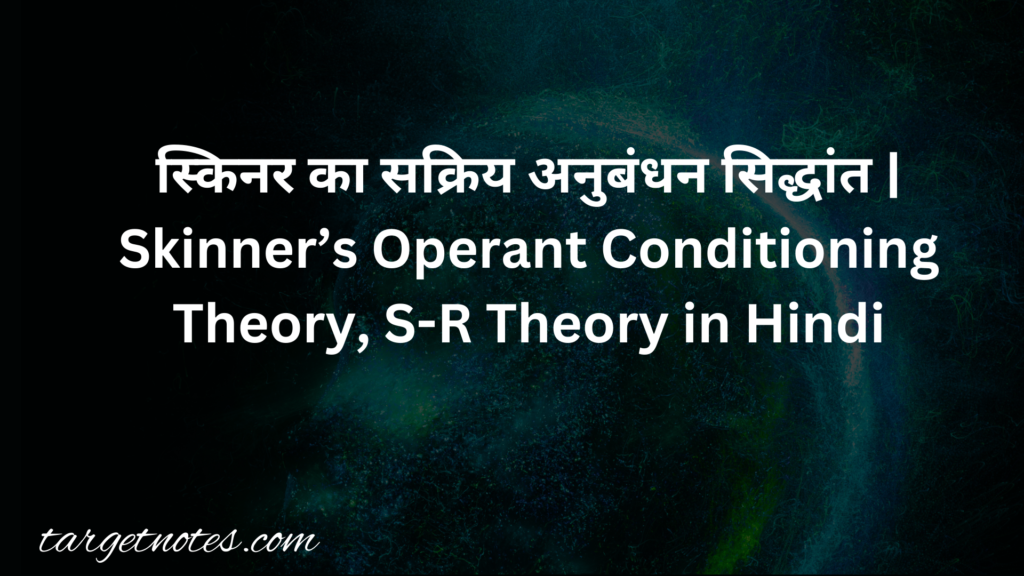
स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत क्या है?
Contents
स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत
स्किनर का क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध- व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बी० एफ० स्किनर द्वारा प्रयोगशाला में पशुओं पर अधिगम के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण प्रयोग किये गये हैं। स्किनर ने अपने प्रयोगों के आधार पर अधिगम के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, उसे अनुबद्ध अनुक्रिया-सिद्धान्त या क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध का सिद्धान्त कहते हैं। बी० एफ० स्किनर ने व्यवहार को दो श्रेणियों में रखा है-
1. प्रतिकृत व्यवहार – ये अनुक्रियाएँ होती हैं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण होती हैं। इनमें एक ज्ञात उद्दीपक एक निश्चित अनुक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे “भोजन” उद्दीपक “लार टपकने” की अनुक्रिया को उत्पन्न करता है।
2. क्रिया-प्रसूत व्यवहार – जब प्राणी के व्यवहार में बिना किसी ज्ञात उद्दीपक के स्वतः स्फूर्त ढंग से अनुक्रिया उत्पन्न होती है तो उसे क्रिया-प्रसूत व्यवहार कहते हैं, अर्थात् वे अनुक्रियाएँ जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण नहीं होर्ती, क्रिया-प्रसूत व्यवहार कहते हैं, अर्थात् वे अनुक्रियाएँ जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण होती, क्रिया-प्रसूत व्यवहार कहलाती हैं।
स्किनर के अनुसार मानव-व्यवहार का तीन चौथाई से भी अधिक अंश क्रिया-प्रसूत व्यवहार की श्रेणी में रखा जा सकता है। स्किनर ने जिस प्रकार के अनुबन्धन का तरीका अपनाया, उसमें प्रााणी द्वारा क्रिया उत्पन्न करने पर विशेष बल दिया। इसके अन्तर्गत अधिगम-स्थिति को इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि जब तक सीखने वाला वांछित व्यवहार न करे, तब तक उसे पुरस्कार न मिले। यहाँ सीखने वाले को यह अवसर दिया जाता है कि वह अधिगम-स्थिति में सक्रियता की भूमिका कर सके।
स्किनर ने अपना प्रारंभिक प्रयोग एक कबूतर पर किया था। भूखे कबूतर ने स्वतः क्रिया द्वारा यह सीख लिया कि दाहिनी ओर सिर घुमाकर चोंच मारने से दाना (प्रबलक) मिल जाता है।
क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध में अनुक्रिया को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें पहले कुछ क्रियाएँ या व्यवहार करना पड़ता है। उसके फलस्वरूप उद्दीपन प्रकट होता है। इसीलिए इसमें अधिगम का स्वरूप अ-उ (R-S) सूत्र में प्रदर्शित करते हैं।
स्किनर के उपर्युक्त प्रयोग से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं-
(1) प्रयोग के आरम्भ में सही अनुक्रिया के बीच कबूतर मनचाहा व्यवहार (जैसे घूमना, इधर-उधर चोंच मारना, बायें सिर घुमाना आदि) करने के लिए स्वतन्त्र है, किन्तु उसे दाना (पुनर्बलक) तभी दिया जाता है जब वह प्रयोगकर्ता द्वारा निर्धारित अन्त्य व्यवहार को करता है।
(2) इस प्रकार के पूर्व-नियोजित कौशल को सिखाने में अधिक समय नहीं लगता।
(3) प्रयोगकर्ता इच्छित व्यवहार होने पर कबूतर को हर बार दाना देता है। मनोवैज्ञानिक शब्दावली में इसे इच्छित अनुक्रिया का पुनर्बलित करना कहेंगे। जब भी सही अनुक्रिया होती है, तब उसे पुनर्बलित किया जाता है, किन्तु गलत अनुक्रिया होने पर उसे दण्ड नहीं दिया जाता है।
क्रिया-प्रसूत अनुबन्धन के अन्तर्गत होने वाले कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ अग्रलिखित हैं-
1. रूपण या व्यवहार रचना-क्रिया- प्रसूत अनुबन्धन में रूपण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगमकर्ता में वांछित व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए समयानुकूल समुचित पुनर्बलन प्रदान करने से यह सम्बन्धित है। रूपण के प्रक्रम में वांछित व्यवहार तक पहुँचने के लिए एक के बाद एक पुनर्बलन दिया जाता है। वांछित व्यवहार अथवा अन्त्य व्यवहार तक अधिगमकर्ता को पहुँचाने के लिए अर्थात् अधिगमकर्ता के व्यवहार का वांछित रूपण करने के लिए स्किनर ने तकनीक विकसित किया है।
उदाहरण के लिए, यदि हम कबूतर को निश्चित स्थान पर चोंच मारकर उत्तोलक दबाना सिखाना चाहते हैं, तब इसके लिए हमें क्रम से व्यवहार के इस रूप तक पहुँचना होगा, जब तक कबूतर अन्त्य व्यवहार न करे अर्थात् उत्तोलक को न दबाये, तक तक प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा। इसके स्थान पर अत्यन्त व्यवहार तक पहुँचने के प्रक्रम में आने वाली प्रक्रियाओं पर हमें ध्यान देना होगा। पहले, जब कबूतर उत्तोलक के समीप आता है, उसे पुनर्बलन देना चाहिए। इससे उसमें उत्तोलक के समीप रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायेगी। तत्पश्चात् जब कबूतर उत्तोलक के अत्यन्त समीप आ जाता है, उसे पुनर्बलन देना चाहिए। फिर जब वह उत्तोलक को दबाता है, तभी उसे पुनर्बलन देना चाहिए।
इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध रीति से एक के बाद एक पद पर पुनर्बलन देने से कबूतर अन्त्य व्यवहार के और समीप आ जाता है और अन्त में उसके व्यवहार को मनोवांछित व्यवहार में रूपान्तरित कर दिया जाता है।
रूपण की प्रक्रिया में अनुबन्धन के निम्नलिखित तीन सिद्धान्त प्रयुक्त होते हैं-
(अ) सामान्यीकरण- अधिगमकर्ता में एक परिस्थति में अर्जित ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति को उसी प्रकार की दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकृत कर प्रयुक्त करने की क्षमता होती है। सामान्यीकरण दो प्रकार का हो सकता है-
(i) उद्दीपन सामान्यीकरण – यह तब होता है जब किसी एक उद्दीपन द्वारा एक अनुक्रिया होती है और उसी प्रकार के किसी अन्य उद्दीपन से भी वही अनुक्रिया हो। उद्दीपन सामान्यीकरण में परिस्थितियाँ या उद्दीपन बदलते हैं, किन्तु अनुक्रिया वही रहती है। उदाहरण के लिए, वाटसन के प्रयोग में एक बालक जोर की आवाज से डरता है, फिर दूध, बिल्ली और यहाँ तक कि रोंयेदार कोट पहने हुऐ अपनी माँ से भी डरता है।
सामान्य घेरलू व्यवहार में भी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे अपने पिता के रूप, रंग एवं पहनावे वाले किसी पुरुष को पापा या पिताजी कह बैठते हैं।
(ii) अनुक्रिया सामान्यीकरण- रूपण की प्रक्रिया में अनुक्रिया सामान्यीकरण का अधिक महत्व है, क्योंकि इसी के सहारे रूपण सम्भव हो पाता है। अनुक्रिया सामान्यीकरण में अनुक्रियाएँ बदलती हैं। उद्दीपन वही रहता है। उदाहरण के लिए स्किनर के प्रयोग में हमने देखा कि अनुक्रिया सामान्यीकरण के द्वारा ही कबूतर उत्तोलक दबाने की क्रिया के समीप धीरे-धीरे पहुँचता है (पहले उत्तोलक के समीप आना, गर्दन दाहिनी ओर घुमाना और अन्त में सही तरीके से चोंच मारना)
(ब) आदत प्रतिस्पर्धा – रूपण की प्रक्रिया में दूसरा सिद्धान्त आदत प्रतिस्पर्धा का है। सही आदत अथवा अनुक्रिया को अन्य अनुक्रियाओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। सही अन्त्य व्यवहार तक होने वाली क्रियाओं की श्रृंखला में प्रत्येक पद पर अन्य व्यवहार भी होते रहते हैं किन्तु सही व्यवहार को पुनर्बलित किया जाता है। दूसरे व्यवहारों को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। व्यवहारों और आदतों की इस होड़ में वांछित व्यवहार को पुनर्बलित कर सफल बना दिया जाता है।
(स) श्रृंखलन- रूपण में अन्तिम व तीसरा सिद्धान्त श्रृंखलन का है। रूपण की प्रक्रिया में व्यवहार का प्रत्येक अंश दूसरे अंश से श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। एक अनुक्रिया करने से जो संकेत मिलता है, वह दूसरी श्रृंखला से अवश्य जुड़ी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कबूतर के प्रयोग में यदि कबूतर अपनी गर्दन सही दिशा में थोड़ा सा भी झुकाता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाता है। इस आदत के पुनर्बलित होने पर यह आदत दृढ़ हो जाती है। यहाँ से अन्त्य व्यवहार तक आने वाली एक-एक क्रिया को एक के बाद एक पुनर्वलित करते हुए श्रृंखलाबद्ध कर दिया जाता है। इस तरह कबूतर का समस्त व्यवहार रूपान्तरित हो जाता है।
प्रभावकारी रूपण के तत्त्व-रूपण की तकनीक से ही हम प्राणी के व्यवहारों को सुनिश्चित उद्देश्यों के अनुरूप बदल सकते हैं। प्रभावकारी रूपण के लिए निम्नलिखित बातों का होना अत्यन्त आवश्यक है-
(i) अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय अनुक्रिया- प्रत्येक पद पर अधिगमकर्ता सक्रियता से भाग लेता है, न कि प्रयोगकर्ता या शिक्षक ।
(ii) तत्काल पुनर्बलन – जब भी अधिगमकर्ता द्वारा सर्वोत्तम व्यवहार होता है, उसे तत्काल पुनर्बलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में सही या वांछित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाता है।
(iii) क्रमिक उपगमन- अधिगमकर्ता पहले जो कुछ भी करता है, उसे पुनर्बलित किया जाता है। अन्त्य व्यवहार तक पहुँचने के लिए जिन-जिन क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें छोटे-छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाता है। हर पद पर पुनर्बलन देते हुए क्रमिक उपगमन के सहारे अधिगमकर्ता को अन्त्य व्यवहार तक पहुँचाया जाता है।
(iv) प्रवीणता – प्रवीणता प्रगति पर आश्रित है। सरल एवं प्रथम पद पर सफल और पुनर्बलित होने के पश्चात् ही अधिगमकर्ता को दूसरा पद दिया जाता है अर्थात् जब तक पहले पद पर वह प्रवीण नहीं हो जाता, तब तक उसे दूसरा नया और पहले पद से जटिल पद नहीं दिया जाता।
2. विलुप्तीकरण-क्रिया- प्रसूत अनुबन्ध के अन्तर्गत होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया विलुप्तीकरण की है। वांछित अनुक्रिया होने पर पुनर्बलन को हटा लेने से या पुनर्बलन न देने से विलुप्तीकरण की प्रक्रिया होती है। मान लीजिए कि चोंच मारने पर दाना देकर इस अनुक्रिया को पुनर्बलित कर सिखा दिया गया है। अब चोंच मारने पर दाना देना बन्द कर दिया जाय तो चोंच मारने पर सीखी हुई अनुक्रिया का विलुप्तीकरण हो जायेगा।
3. सहज पुनः प्राप्ति- विलुप्तीकरण के पश्चात् यदि अधिगमकर्ता को प्रायोगिक परिस्थिति से कुछ समय के लिए हटा दें और पुनः वापस लाने पर सीखी हुई अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन दे दिया जाय तो पुराना अनुबन्धित अधिगम सहज ही पैदा हो जाता है। इसी घटना को अनुबन्ध के सिद्धान्त में सहज पुनः प्राप्ति कहते हैं।
क्रिया-प्रसूत आदत की सहज पुनः प्राप्ति इन बातों पर निर्भर करती है। विलुप्तीकरण के पश्चात् कितना समय बीता है, पहले अधिगम के समय कितनी बार पुनर्बलन दिया गया था। अधिगम के समय दो पुनर्बलन के बीच समय का कितना अन्तराल दिया गया था।
4. पुनर्बलन – पुनर्बलन का संप्रत्यय क्रिया-प्रसूत अधिगम का प्राण है। इसे भली-भाँति समझे बिना क्रिया-प्रसूत अधिगम को समझना सम्भव नहीं है। पुनर्बलित करना सुदृढ़ करना है। पुनर्बलन किसी क्रिया के पश्चात् घटने वाली एक ऐसी घटना है जो उस क्रिया को पुष्ट करती है अर्थात् उस क्रिया के पुनः होने की सम्भावना बढ़ जाती है। किसी भी प्राणी को हम दो प्रकार से
पुनर्बलित कर सकते हैं, कुछ देकर या कुछ उसके पास से हटाकर। अधिगमकर्ता को कुछ देकर पुनर्बलित करने को धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अधिगमकर्ता के पास से कुछ हटाकर पुनर्बलित करने को ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं।
स्किनर ने पुनर्बलन के व्यवहार को नियन्त्रित करने की एक विधि माना है, शास्त्रीय अनुबन्धन के प्रतिपादकों की तरह S-R सम्बन्ध को उत्पन्न करनें वाली एक काल्पनिक युक्ति नहीं। जिस घटना या वस्तु के द्वारा पुनर्बलन होता है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन वे घटनाएँ हैं जिनके कारण अनुक्रिया की गति में वृद्धि होती है। स्किनर क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध के सिद्धान्त का प्रयोग विद्यालयी अधिगम में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह उसने अभिक्रमित अधिगम की प्रणाली में करके दिखाया। स्किनर ने प्रचलित शिक्षा-पद्धति की निम्नलिखित कमियों का उल्लेख किया है-
(i) अवांछित उद्दीपनों से व्यवहार का नियन्त्रण- विद्यालयों का वातावरण दुःखद अनुभवों तथा भय से भरा होता है।
(ii) व्यवहार और पुनर्बलन के बीच अधिक अन्तर- वर्तमान में विद्यालयों में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि सही व्यवहार को तुरन्त पुनर्बलित नहीं किया जा सकता। इसके अभाव में अधिगम की गति पर पुनर्बलन का प्रभाव नहीं पड़ पाता। अत्यन्त विलम्ब से दिया गया पुनर्बलन प्रभावहीन होता है।
(iii) तारतम्य का अभाव – वर्तमान शिक्षा-पद्धति में विषय-वस्तु को छोटे-छोटे पदों में क्रमबद्ध करके रखने की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक पद पर पुनर्बलन नहीं दिया जा सकता है।
(iv) स्पष्ट उद्देश्यों का अभाव – कक्षा-शिक्षक प्रत्येक पाठ के व्यावहारिक उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट नहीं होते। उन्हें पता नहीं होता कि वे पाठ को किन व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पढ़ा रहे हैं।
उपर्युक्त सभी दोषों को दूर करने में स्किनर ने क्रिया-प्रसूत अनुबन्ध पर आधारित अभिक्रमित अधिगम शिक्षण दूर करने का स्पष्ट प्रयास किया है।
Important Link…
- अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार के सिद्धान्त (स्रोत)
- अधिकार की सीमाएँ | Limitations of Authority in Hindi
- भारार्पण के तत्व अथवा प्रक्रिया | Elements or Process of Delegation in Hindi
- संगठन संरचना से आप क्या समझते है ? संगठन संरचना के तत्व एंव इसके सिद्धान्त
- संगठन प्रक्रिया के आवश्यक कदम | Essential steps of an organization process in Hindi
- रेखा और कर्मचारी तथा क्रियात्मक संगठन में अन्तर | Difference between Line & Staff and Working Organization in Hindi
- संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले संयोगिक घटक | contingency factors affecting organization structure in Hindi
- रेखा व कर्मचारी संगठन से आपका क्या आशय है? इसके गुण-दोष
- क्रियात्मक संगठन से आप क्या समझते हैं? What do you mean by Functional Organization?